‘एक भ्रांति है कि किसी नामचीन आलोचक के फ़तवे से कोई कहानी महान हो सकती है। वह कालजयी तो अपनी आंतरिक गुणवत्ता से ही बनती है।’–जन्मशती वर्ष में अमरकांत को याद करते हुए उनकी कालजयी कहानी ‘ज़िंदगी और जोंक’ पर चंचल चौहान की सुचिंतित टिप्पणी:

अमरकांत का यह जन्मशती वर्ष है। हिंदी जगत उन्हें बहुत आदर से याद करेगा। मैं भी उनकी स्मृति को नमन करता हूं। हिंदी साहित्य के पाठकों को यह मालूम है कि ‘नयी कहानी’ आंदोलन के दौर में यथार्थवादी धारा के अनेक रचनाकारों में अमरकांत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यथार्थवाद ही उनकी कहानी कला का मूल स्रोत है। उनके कई समकालीन कथाकार किसी न किसी वैचारिकी से जीवन जगत देखते और उसे उसी नज़र से कहानी में चित्रित करते थे। कुछ अस्तित्ववादी जीवनदर्शन से रचनाशक्ति हासिल कर रहे थे तो कुछ मार्क्सवाद की वैचारिकी से दुनिया देखते थे। अमरकांत की रचनाओं में उस तरह की किसी वैचारिकी की झलक नहीं मिलती। वे इस अर्थ में प्रगतिशील ज़रूर थे कि वे अपने समय के सामाजिक यथार्थ को अपने पात्रों के माध्यम से सामने लाते थे। उन्होंने ढेर सारी कहानियां लिखीं जो दो खंडों में प्रकाशित हैं। उनकी कहानियों में समाज के विभिन्न वर्गों के इंसान दिखायी देते हैं। अनेक कहानियों में निम्न मध्यवर्ग की आशाएं आकांक्षाएं, उनकी क्षुद्रताएं और उनके अच्छेपन की तस्वीरें मिल जायेंगी। मसलन ‘डिप्टी कलक्टरी’ में जहां निम्नमध्य वर्ग की ऐसी ख्वाहिशें दिखती हैं कि ‘हर ख्वाहिश पे दम निकले’ तो दूसरी ओर ‘ज़िंदगी और जोंक’ में या ‘लाखो’ में उसी वर्ग की क्षुद्रताएं नज़र आती हैं। ‘रिश्ता’ कहानी में सांप्रदायिक सद्भाव की प्रेमचंदीय तस्वीर बहुत सुकून देती है। ‘दोपहर का भोजन’ में निम्नमध्यवर्ग की खस्ता हालत का चित्र है तो ‘पक्षधरता’ कहानी में समृद्ध निम्नमध्यवर्ग के ‘एट होम’ की तस्वीर है। अमरकांत की कहानी कला सामाजिक जीवन के इसी तरह के विविध अंशों को चित्रित करने में निखरी है।
हिंदी कहानी की विकास यात्रा में कुछ कालजयी रचनाएं आती रही हैं और अभी भी इस तरह की संभावनापूर्ण कहानियां दिख जाती हैं। यह एक भ्रांति है कि किसी नामचीन आलोचक के फ़तवे से कोई कहानी महान हो सकती है। वह कालजयी तो अपनी आंतरिक गुणवत्ता से ही बनती है। ‘बात बोलेगी हम नहीं’। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है चंद्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ की अमर कहानी, ‘उसने कहा था’। मुंशी प्रेमचंद की तो कई कहानियां बहुचर्चित रही आयी हैं। कुछ पर फ़िल्में बनीं, कुछ का नाट्यरूपांतरण हुआ, टी वी सीरियल चले, मगर ‘कफ़न’ कालजयी रचना के रूप में अपना अलग स्थान पा गयी। नयी कहानी के दौर में भी हर रचनाकार की कोई न कोई कहानी हिंदी पाठक समुदाय की स्मृति में रच बस गयी है। राजेंद्र यादव की ‘टूटना’, कमलेश्वर की ‘खोयी हुई दिशाएं’, भीष्म साहनी की ‘चीफ़ की दावत’, निर्मल वर्मा की ‘परिंदे’, मन्नू भंडारी की ‘यही सच है’, कृष्णा सोबती की ‘बादलों के घेरे’, शेखर जोशी की ‘कोसी का घटवार’, फणीश्वर नाथ ‘रेणु’ की ‘तीसरी कसम’ (सूची काफ़ी लंबी है) आदि अनेक रचनाएं इसी श्रेणी में आती हैं।
अमरकांत की ‘ज़िंदगी और जोंक’ भी एक कालजयी रचना है। मैं कालजयी रचना उसे मानता हूं जो सहृदय पाठक या आलोचक को रचना में रचे बसे संश्लिष्ट यथार्थ की व्याख्या करने के लिए उकसाती है। इकहरे यथार्थ या सतही यथार्थ की कहानियां समय के प्रवाह में डूब जाती हैं, उनमें किसी आलोचकीय भाष्य की संभावना नहीं दिखती। आइए, ‘ज़िंदगी और जोंक’ के सौंदर्य का विश्लेषण करें।
‘ज़िंदगी और जोंक’ अमर कांत की ऐसी कहानी है जिसमें निहित संश्लिष्ट यथार्थ उसके भाष्य की संभावना के द्वार खोल देता है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र रजुआ है। वह आज़ादी के बाद के भारत में दर दर भटकते निर्धन व्यक्ति का प्रतीक है। वह न तो संगठित क्षेत्र का क्रांतिकारी सर्वहारा मज़दूर है और न कृषि व्यवस्था में पसीना बहाता खेतिहर मज़दूर। वह क़स्बे के एक मुहल्ले में निम्न मध्यवर्ग के टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर आज़ाद भारत का ग़रीब है जिसे उसकी जिजीविषा गांव से शहर की ओर खींच लायी है। अमरकांत नयी कहानी के अनेक रचनाकारों की तरह अपनी कहानी में सांकेतिकता और नवीन बिंबयोजना का सुंदर इस्तेमाल करते हैं। इस कहानी में भी कहानी के शीर्षक से ही ‘जोंक’ के बिंब से यह संकेत दे दिया है कि कहानी के केंद्र के ग़रीब की ज़िंदगी पशुजीवन से बेहतर नहीं है। कहानी की बुनावट में भी पशुओं के बिंब बार बार आते हैं। मुहल्ले के शिवनाथ बाबू रजुआ को पनाह दे देते हैं। मगर उनके घर के लोग रजुआ को साड़ी चुराने के आरोप में पीटने लगते हैं। शिवनाथ बाबू गुस्से में उसे ‘हरामी का पिल्ला’ कहते हैं। वे वाचक को बताते हैं कि उन्होंने रजुआ को पनाह दी, पर उन्हें क्या पता था कि वह चोर निकलेगा। वे कहते हैं कि ‘लालची कुत्तों की तरह इधर-उधर घूमा करता था।‘ रजुआ की सभी ने खूब पिटाई की, मगर थोड़ी देर में पता लग गया कि साड़ी तो घर में ही थी, तो उसकी पिटाई बंद हो गयी। मगर शिवनाथ बाबू ने इसके लिए कोई पश्चाताप नहीं किया, वाचक से कह दिया कि ‘इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गयी है, पर कोई बात नहीं। चमार-सियार डांट-डपट पाते ही रहते हैं।’ भारत की मनुवादी मानसिकता और निम्नमध्यवर्गीय अहं अमरकांत की इस कहानी में उजागर होता गया है। अमरकांत इस कहानी में बार बार इस यथार्थ को कलात्मक रूप देने के लिए पशु-इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। रचनाकार इस तरह की बिंबयोजना से यह दर्शाता है कि आज़ादी के बाद के भारत में ग़रीब की ज़िंदगी पशु जैसी ही थी। वाचक कहता है कि
बचा हुआ बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय-भैंसों को दे दिया जाता, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देतीं कि जाकर भिखमंगे को दे आयें।
इसी तरह आगे कहानी का वाचक उसके बारे में बताता है कि पिटाई के बाद उसने शिवनाथ बाबू के यहां जाना बंद कर दिया। मुहल्ले के दूसरे लोग उससे काम लेने लगे तो एक दिन शिवनाथ बाबू ने उसे रास्ते में रोककर समझाया कि वह फिर से उन्हीं के पास काम करने लगे। उन्होंने कहा, ‘दर-दर भटकता रहता है। कुत्ते-सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़, आराम से यहीं रह और दोनों जून भरपेट खा।’ वह राज़ी हो गया । वह उनके यहां स्थायी रूप से रहने लगा। उन्होंने ही उसे ‘रजुआ’ नाम दिया। मगर मुहल्ले वालों को यह कारनामा नागवार गुज़रा। वे भी उससे काम करवा लिया करते थे, सो वह साधन हाथ से निकल गया। फिर भी वे उसे लालच दे कर अपना छोटा मोटा काम करवाने लगे थे। धीरे धीरे वह सारे मुहल्ले का ही नौकर हो गया था।
जमनालाल के लड़के जंगी ने उसे लकड़ी खरीद कर लाने का काम सौंपा तो वह शिवनाथ बाबू के घर पर व्यस्तता के चलते नहीं कर पाया। जंगी ने ‘दो थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिये, फिर गरजकर बोला- ‘सुअर, धोखा देता है?’ इस तरह अमरकांत बार बार उसके लिए पशु इमेजरी की रचना करते हैं।
वाचक बताता है कि रजुआ उनके यहां भी आने लगा था क्योंकि उनकी पत्नी भी कुछ न कुछ काम करवा कर कुछ खाने को दे देती थीं। वाचक ने एक दिन देखा कि ‘उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा-सा अचार था और वह सूअर की भांति चापुड़-चापुड़ खा रहा था।’ धीरे धीरे रजुआ मुहल्ले में रम गया था, सभी से हिल मिल गया था। अब भोजन की समस्या पहले जैसी नहीं थी। जैसा काम वैसा दाम जैसा कुछ न कुछ मिल जाता था।
फ्रायड ने बताया था कि इंसान की मूलवृत्ति ‘लिबिडो’ यानी कामवासना है, युंग ने इसका खंडन करने हुए कहा कि मूल वृत्ति तो जिजीविषा है। रजुआ में इन्हीं दोनों वृत्तियों का विकास देखा जा सकता है। ये दोनों वृत्तियां पशुजीवन में भी तो हैं, मनुष्य को इन दोनों के साथ कुछ रचनात्मक करना होता है। रजुआ के पास मनुष्य बनने की वह साधना संभव नहीं थी। इसलिए अमरकांत उसके लिए बार बार पशु इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। पतुआ की बहू से रजुआ जब मज़ाक करता हुआ हंसी ठिठोली करता है तो वह उसे डांट देती है। उसकी डांट से ही वह खुश हो जाता है। वाचक लिखता है कि उसने, ‘ऐसी किलकारियां लगायीं जैसे घास चरता हुआ गदहा अचानक सिर उठाकर ढीचूं-ढीचूं कर उठता है।’ कहानी आगे बताती है कि ‘फिर तो यह उसकी आदत हो गयी। सारे मुहल्ले की छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया था। उनको देखकर वह कुछ हल्की-फुल्की छेड़ख़ानी कर देता और तब वह गधे की भांति ढीचूं-ढीचूं कर उठता।’ रजुआ में जिजीविषा के साथ ‘लिबिडो’ का प्रस्फुटन हो चला था।
धीरे धीरे रजुआ मुहल्ले में रच बस गया। वह खंडहर में नहीं, कहीं भी रह जाता। खाने पीने का जुगाड़ हो गया, काम के अनुसार कुछ मज़दूरी भी मिलने लगी। अमरकांत उसके इस विकास के साथ उसमें कामवासना का विकास दिखाते हैं। कहानी का वाचक उसे मुहल्ले की औरतों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए दिखाता है। इसी क्रम में वाचक उसे रेलवे प्लेटफार्म पर नंगी पागल स्त्री से बात करते हुए चित्रित करता है। स्टेशन पर पुलिस के सिपाही उसे वहां से भगाते हैं : ‘भाग जा साले, गिद्ध की तरह न मालूम कहां से आ पहुंचा…’। बाद में वह उसी पागल स्त्री को क्वार्टरों की छत पर ले जाता है। उसे खाना खिलाता है। रात में जब वह पागल स्त्री के पास जाता है तो उसके पास कोई और आदमी लेटा हुआ होता है जो रजुआ की पिटाई करता है। वाचक बताता है कि उस घटना के बाद ‘उसका स्त्रियों के साथ छेड़ख़ानी करके गधे की भांति हिचकना-किलकना बंद हो गया।’
अमरकांत रजुआ के जीवन में आने वाले अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों ही चित्रित करते हैं, कभी खुशी कभी ग़म। रजुआ से वह ‘रज्जू भगत’ बन जाता है। फिर वह हैज़े की महामारी की चपेट में आ जाता है, वाचक उसे मरणासन्न देखकर अस्पताल में भरती करवा कर उसकी जान बचा लेता है। फिर उसे भयानक खुजली हो जाती है।
एक दिन एक लड़का वाचक के पास उसके मरने की ख़बर रजुआ के भाई के पास भेजने के लिए एक पोस्टकार्ड ले कर आता है। वाचक उसके मरने की ख़बर लिखकर पोस्टकार्ड उस लड़के को दे देता है। वाचक उसके मरने के समाचार से उसके बारे में सोचने लगता है। वह कहता है, ‘चूंकि वह मरना न चाहता था, इसलिए जोंक की तरह ज़िंदगी से चिमटा रहा। लेकिन लगता है, ज़िंदगी स्वयं जोंक-सरीखी उससे चिमटी थी और धीरे-धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद तक पी गयी।’ मगर रजुआ मरा नहीं था, उसने प्रकट हो कर वाचक को असलियत बतायी, ‘बात यह हुई सरकार कि मेरे सिर पर एक कौवा बैठ गया था। हुज़ूर कौवे का सिर पर बैठना बहुत अनसुभ माना जाता है। उससे मौअत आ जाती है!’
पशु इमेजरी का इस तरह का अदभुत प्रयोग करते हुए अमरकांत कहानी का अंत भी उसी ‘जोंक’ के बिंबप्रयोग से करते हैं :
उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह ज़िंदगी से जोंक की तरह चिमटा था—लेकिन जोंक वह था या ज़िंदगी?
‘दोपहर का भोजन’ कहानी में भी पशु इमेजरी का प्रयोग सधे हुए ढंग से अमरकांत करते हैं, ‘सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आये और वहीं से वह भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका-घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही।’ इसी तरह चंद्रिका प्रसाद के लिए भी इसी तरह का प्रयोग किया, ‘दो रोटियां, कटोरा-भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक-एक ग्रास को इस तरह चुभला-चबा रहे थे, जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है।’ पूरे घर की हालत को भी पशुइमेजरी से अमरकांत चित्रित करते हैं। ‘सारा घर मक्खियों से भन-भन कर रहा था।’
‘ज़िंदगी और जोंक’ कहानी का अंत पशु इमेरजरी के साथ एक सवालिया निशान से होता है। यह संकेत उस दौर के यथार्थ को लेकर है। नयी कहानी के दौर की असमंजस की चेतना जिसे भारतभूषण अग्रवाल ने ‘पथहीन’ कविता में, ‘अंतरात्मा अनिश्चय-संशय-ग्रसित’ कहा था, हिंदी साहित्य में रची बसी थी। क्रांति का अगुआ दस्ता भारत का सर्वहारा वर्ग भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद की वैज्ञानिक विचारधारा की मदद से तय नहीं कर पा रहा था कि भारत की सत्ता किन वर्गों के हाथ में आयी थी, उसका कोई पार्टी प्रोग्राम यानी आधारभूत दस्तावेज़ भी नहीं बन पाया था, यानी वह भी असमंजस की हालत में था। धीरे धीरे भारतीय समाज की असलियत सामने आने लगी तो पिछली सदी के सत्तर के दशक के बाद वही ‘रजुआ’ उदयप्रकाश की कहानी में ‘टेपचू’ के रूप में दिखायी देने लगा। उदय प्रकाश का टेपचू भी अमरकांत के रजुआ की तरह पशु इमेजरी से चित्रित होता है लेकिन वह क्रांतिकारी सर्वहारा के रूप में विकसित होता हुआ एक मिथक का दर्जा हासिल कर लेता है। यह चेतना उस दौर की उपज थी जब हिंदी साहित्य का हर उभरता हुआ लेखक भारतीय समाज के विकास के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद के दर्शन पर आधारित समाज संरचना का सपना देख रहा था। यह सपना मरा नहीं, टेपचू की तरह अमर है। अब वह अमरकांत का रजुआ नहीं है। जब तक शोषण-पाप का परंपराक्रम जारी रहेगा, क्रांतिकारी सर्वहारावर्ग, उसका दर्शन, राजनीति और दुनिया को शोषणमुक्त बनाने का सपना भी ज़िंदा रहेगा। मुक्तिबोध के शब्दों में, ‘यह भवितव्य अटल है/ इसको अंधियारे में झोंक न सकते।’
dr.chnchlchauhan@gmail.com

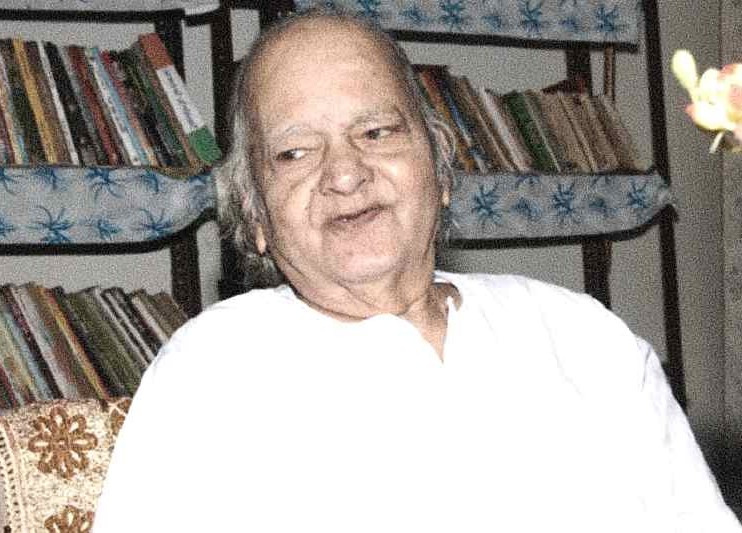







यह कहानी तो पहले भी पढी थी लेकिन इस ढंग से देख नहीं पाया था. बेहतरीन आलोचकीय दृष्टि के लिए चंचल चौहान जी को बधाई.
I need Naya Path
For reading
अब यह प्रिंट में नहीं है. ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं.