भाषा का मसला पहले से भी, और इन दिनों विशेष रूप से, विवादों में रहा है। हमें कैसी हिंदी चाहिए, हिंदी को किस तरह के संरक्षण की ज़रूरत है, उसे अहिंदी भाषी इलाक़ों के लिए पाठ्यक्रमों और सरकारी कामकाज में अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं—ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन पर हम अक्सर उलझते हैं, और खुद में भी उलझे रहते हैं। जवरीमल्ल पारख का यह लेख इन मुद्दों पर एक सुलझी हुई राय सामने रखता है जिसका संबंध इस बात से भी है कि भाषा के सवाल को उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ जोड़ कर देखा है। इसलिए उनके सुझाव बहुत व्यावहारिक हैं। कुछ लोगों के लिए वे बहसतलब हो सकते हैं। बहस के लिए स्वागत है!

मेरी मातृभाषा मारवाड़ी है जिसे चाहें तो आप राजस्थानी भी कह सकते हैं। हालाँकि राजस्थानी के कई रूप हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, धुन्धरी, मेवाती, शेखावटी, हाड़ौती और शायद कुछ और भी। मारवाड़ी राजस्थान की पुरानी रियासत मारवाड़ की भाषा है, और इसी वजह से वह मारवाड़ी कहलाती है। मारवाड़ का सबसे बड़ा शहर जोधपुर है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। यह मारवाड़ी जोधपुर सहित पूरे मारवाड़ में बोली जाती रही है और आज भी बोली जाती है। मारवाड़ी इसलिए मेरी मातृभाषा है कि मैंने अपने माता और पिता से उनका अनुकरण करते हुए सबसे पहले वही भाषा सीखी थी। मेरी माँ जो अभी नब्बे साल की हैं, जीवन भर मारवाड़ी ही बोलती रही हैं। वे हिंदी नहीं बोल सकतीं। हिंदी समझने में भी उन्हें कठिनाई होती है। मेरे माता-पिता जिस तरह की मारवाड़ी बोलते हैं, मैं और मेरे भाई-बहन वैसी ही मारवाड़ी बोलते हैं। फ़र्क़ यह है कि मेरी माँ की भाषा में हिंदी से आये शब्द बहुत कम इस्तेमाल होते हैं जबकि हमारी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी से लिये गये बहुत से शब्द मारवाड़ी बोलते हुए भी आ जाते हैं। माँ की भाषा ज़्यादा मारवाड़ी इसलिए है कि वह कभी स्कूल नहीं गयी। लेकिन मैंने महसूस किया कि माँ की मारवाड़ी में जोधपुर शहर में प्रचलित बहुत से ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो दूसरी भाषाओँ से शहरी मारवाड़ी में घुलमिल गये हैं जबकि गाँवों की मारवाड़ी में ऐसे शब्द बहुत कम होते थे।
सामाजिक जीवन से लुप्त होती मातृभाषा
हिंदी मैंने तब सीखी जब स्कूल पढ़ने गया। हिंदी से मेरा परिचय ही तब हुआ जब मैं स्कूल में भर्ती हुआ। वहाँ शिक्षा का माध्यम हिंदी था, मारवाड़ी नहीं। पढ़ाने वाले अध्यापकों की मातृभाषा भी मारवाड़ी थी लेकिन वे हिंदी में पढ़ाते थे। धीरे-धीरे पढ़ने, लिखने और बोलने की भाषा हिंदी हो गयी। कुछ इस तरह कि घर-परिवार के सदस्यों के साथ मारवाड़ी संवाद की भाषा थी और घर से बाहर हिंदी। लेकिन प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में प्रवेश लिया तब कुछ छात्र और अध्यापक वे भी आये जिनकी मातृभाषा मारवाड़ी नहीं थी। कई अध्यापक उत्तरप्रदेश के थे, हेड मास्टर बंगाली थे और कुछ साथ पढ़ने वाले भी जोधपुर-मारवाड़ के न होकर राजस्थान के किसी और हिस्से के थे या किसी और राज्य के थे। उनकी भाषा मारवाड़ी नहीं थी। इसलिए अब धीरे-धीरे घर से बाहर की संपर्क भाषा सभी के साथ हिंदी हो गयी। मारवाड़ी घर-परिवार तक ही सीमित रह गयी। कक्षा तीन से अंग्रेजी भी शिक्षा के एक विषय के रूप में शामिल हो चुकी थी। लेकिन वह हिंदी की तरह संपर्क और संवाद की भाषा नहीं बनी।
हायर सेकेंडरी करने के बाद जोधपुर पोलिटेक्निक में प्रवेश लिया। वहाँ शिक्षा का माध्यम एक-दो साल पहले ही अंग्रेजी से हिंदी हुआ था। लेकिन वहाँ कक्षा में अध्यापक हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिला-जुला उपयोग करते थे। कुछ केवल अंग्रेजी में पढ़ाते थे। पाठ्यपुस्तकें ज़्यादातर अंग्रेजी में थीं। हिंदी में अभी किताबें तैयार नहीं हुई थीं। स्कूल में माध्यम हिंदी था, इसलिए परीक्षा देने का माध्यम यहाँ भी हिंदी ही रहा। अगर हायर सेकेंडरी में कुछ अंक ज़्यादा आते और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश हो जाता तो माध्यम अंग्रेजी ही होता और परीक्षा भी अंग्रेजी में ही देनी होती। जैसे मेरे छोटे भाई को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही अपनाना पड़ा जबकि स्कूल में उसका माध्यम भी हिंदी ही था। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों को शुरू में अंग्रेजी माध्यम अपनाने में परेशानी होती थी लेकिन धीरे-धीरे उन्हें अंग्रेजी में लिखने और बोलने की आदत पड़ जाती है। मेरे साथ इसलिए बदलाव नहीं हुआ कि पोलिटेक्निक करने के बाद बी ए ऑनर्स और एम ए हिंदी साहित्य विषय के साथ किया और इसी वजह से अध्ययन और अध्यापन का माध्यम भी हिंदी ही रहा। पीएच-डी उपाधि के लिए शोध प्रबंध भी हिंदी में ही लिखा हालाँकि इस दौरान बहुत कुछ अंग्रेजी में भी पढ़ा।
हिंदी का अध्यापक होने के कारण आगे भी पढ़ने-लिखने और पढ़ाने का माध्यम हिंदी ही रहा। अमरोहा में नौकरी करते हुए मारवाड़ी पीछे छूट गयी। लेकिन मेरी हिंदी बोलने पर मारवाड़ी का असर था जो मुझे तो कम दिखायी देता था लेकिन अमरोहा के विद्यार्थियों को बहुत अधिक दिखायी देता था और मेरे उच्चारण पर वे हँसते थे। कोशिश करने से काफ़ी हद तक सुधार हुआ। पत्नी भी मारवाड़ी परिवार से थी। लेकिन उनके पिता नौकरी के सिलसिले में मारवाड़ से बाहर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और दिल्ली में रहे, इसलिए पत्नी की हिंदी पर मारवाड़ी का असर लगभग नहीं था। पहले दिन से हमारे बीच के संवाद की भाषा हिंदी बनी। मैंने सचेत रूप से तय किया कि हम आपस में हिंदी में बात करेंगे ताकि हमारे घर-परिवार और बाहर की भाषा हिंदी रहे और उस पर मारवाड़ी का असर कम से कम हो। मारवाड़ी का असर इसलिए अखरता था कि जब किसी हरियाणवी या बिहारी की हिंदी सुनता तो वह मुझे वैसे ही चुभती थी जैसे मेरी हिंदी पर मारवाड़ी का असर दूसरों को चुभता था। किसी पंजाबी, बंगाली या दक्षिण भारतीय की हिंदी में उच्चारणगत दोष अपेक्षाकृत कम चुभता था, क्योंकि वे उन प्रदेशों के नहीं थे जिसे हिंदी प्रदेश कहा जाता है। हमारी ज़िंदगी में से मारवाड़ी का उपयोग सीमित होता गया। मैं और मेरी पत्नी अपने घर-परिवार के उन सदस्यों से अब भी मारवाड़ी में बात करते थे जिनसे पहले भी हम मारवाड़ी में बात करते थे। इसका दिलचस्प पहलू यह था कि जिनसे हम मारवाड़ी में बात करते थे, वे अपने मित्रों और परिचितों से हिंदी में बात करते थे।
हमारे दोनों बच्चे मुख्य रूप से दिल्ली में पले-बढ़े, इसलिए उन्हें मारवाड़ी सुनने का अवसर बहुत कम मिला। उन्होंने मारवाड़ी धीरे-धीरे सुनकर समझना तो सीख लिया था लेकिन बोलने में छोटे-छोटे दो-चार वाक्यों से वे आगे नहीं बढ़ सके। बच्चों के स्कूली जीवन में हिंदी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। यानी कि जब मैं स्कूल में पढता था तब शिक्षा का माध्यम हिंदी था और अंग्रेजी एक विषय मात्र। लेकिन अब बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया और हिंदी एक विषय मात्र। मेरे जीवन में साहित्य, सिनेमा और समाचार की भाषा मुख्य रूप से हिंदी थी। हालाँकि हिंदी के साथ अंग्रेजी का अखबार भी मँगाने लगा था। लेकिन बच्चों के लिए साहित्य, सिनेमा और मीडिया की मुख्य भाषा अंग्रेजी हो गयी। वजह यह थी कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, इसलिए अंग्रेजी उनके लिए ज़्यादा सहज हो गयी थी जो मेरे और मेरी पत्नी के लिए नहीं थी। टेलीविज़न पर वे तरह-तरह के कार्यक्रम भी अंग्रेजी में देखने लगे क्योंकि बच्चों के मनबहलाव के प्रोग्राम हिंदी में बहुत कम बनते थे, हिन्दी के लोकप्रिय धारावाहिक ज़्यादातर सास-बहू के घरेलू झगड़ों से सम्बंधित थे जिनमें बच्चों की दिलचस्पी नहीं थी। फ़िल्में ज़रूर अंग्रेजी और हिंदी दोनों की देखते थे। इसलिए मनोरंजन की दुनिया भी काफ़ी हद तक बदल गयी थी।
यहाँ पूछा जा सकता है कि हमने अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? इसका प्रतिप्रश्न यह है कि क्यों पढ़ाते? हमारी पीढ़ी और हमारे बच्चों की पीढ़ी के बीच जो बीस साल से ज़्यादा का अंतराल था, उस दौरान बहुत कुछ बदल चुका था। हमारे समय में ज़्यादातर स्कूल सरकारी और हिंदी माध्यम के थे, और जो सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल थे, वे भी ज़्यादातर हिंदी माध्यम के थे। इन दोनों तरह के स्कूलों का स्तर कुल मिलाकर अच्छा था। लेकिन हमारे बच्चों के समय तक आते-आते (1970-80 के आसपास) सरकारी स्कूलों में तेज़ी से गिरावट होने लगी। अर्धसरकारी स्कूल जो कल तक हिंदी माध्यम के थे, वे भी अंग्रेजी माध्यम में बदलने लगे। नये प्राइवेट स्कूल तेज़ी से खुलने लगे जो अंग्रेजी माध्यम के थे और उनका स्तर निश्चय ही हिंदी माध्यम के स्कूलों से प्रायः बेहतर होता था। दूसरा बड़ा अंतर यह आ रहा था कि संयुक्त परिवार टूट रहे थे। हमारे भाई और बहनें नौकरी के लिए या शादी करके न केवल संयुक्त परिवार से दूर जा रहे थे, उनकी आय के स्रोत भी अलग-अलग और कम-ज़्यादा होते थे। एक संयुक्त परिवार की जगह कई एकल परिवार बन गये थे और वे परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर ज़्यादा जागरूक हो गये थे, इसलिए वे अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में पढ़ाना चाहते थे। एक और बात यह थी कि हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में जाने पर जो कठिनाइयाँ हमारी पीढ़ी को झेलनी पड़ी थीं, हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को वही सब कुछ सहन करना पड़े। लेकिन क्या इससे यह नतीजा निकलना उचित होगा कि भाषा के बदलाव की प्रक्रिया एक आधुनिक फिनोमिना है? क्या मध्ययुग में बदलाव नहीं होते थे? मारवाड़ और उसके आसपास के इलाक़ों के मध्ययुगीन दौर से इसे समझा जा सकता है।
मध्यकालीन दौर और भाषाओँ में बदलाव
जितनी जानकारी मुझे आज है, उसके अनुसार हमारे परिवार में भाषा के बदलाव की यह प्रक्रिया तीन पीढ़ी पहले शुरू हो चुकी थी और मेरे बाद की दो पीढ़ियों में भी दिखायी दे रही है। मारवाड़ जो एक बड़ी रियासत थी, उस पर कभी भी मुग़लों का शासन नहीं रहा। इसलिए उन्हें राजकाज के कामों के लिए फ़ारसी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। उनका ज़्यादातर काम मारवाड़ी में ही होता था और लिखने के लिए नागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन दिल्ली दरबार से भी उन्हें संपर्क और संवाद रखना होता था और इसके लिए फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था जो अकबर के समय दिल्ली की राजकाज की भाषा बन गयी थी। अकबर ने फ़ारसी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था हालाँकि मुग़लों की मातृभाषा तुर्की थी। लेकिन फ़ारसी तुर्की से ज़्यादा विकसित और प्रतिष्ठित भाषा थी। इस भाषा में बड़े-बड़े कवि और विद्वान हो चुके थे। शायद यही वजह थी कि अकबर ने फ़ारसी को राजभाषा बनाया और अंग्रेजों का शासन स्थापित होने से पहले तक फ़ारसी राजभाषा बनी रही। फ़ारसी के इसी महत्त्व के कारण दिल्ली पर जब तक मुग़लों का शासन रहा, तब तक राजभाषा और अभिजात भाषा के रूप में फ़ारसी का बोलबाला रहा। लेकिन देशी रजवाड़ों ने पहले की तरह अपनी ही स्थानीय भाषा में काम करना जारी रखा। मारवाड़ में आम आदमी ही नहीं, सरकारी कामकाज भी मारवाड़ी भाषा में होता था और इसके लिए नागरी लिपि का इस्तेमाल होता था। इन रजवाड़ों का दिल्ली से काफ़ी वास्ता पड़ता था, इसलिए उनके दरबार में कई ऐसे विद्वान्, वकील और मुंशी नियुक्त किये जाते थे जो फ़ारसी जानते थे। इसके लिए संभव है बाहर से विद्वान बुलाये भी जाते रहे हों और यह भी मुमकिन है कि कुछ पढ़े-लिखे परिवारों ने फ़ारसी सीखी हों। जैसे कायस्थ, पंडित और अपवाद रूप में बनियों ने भी फ़ारसी सीखी होगी। लेकिन आम लोगों के बीच संपर्क भाषा और शासन-प्रशासन की भाषा स्थानीय भाषा (मारवाड़ के लिए मारवाड़ी) ही रही। फ़ारसी से इन देशी रियासतों की दूरी बनी रही। लेकिन लश्कर की भाषा और बाज़ार की भाषा के रूप में खड़ी बोली का व्यवहार बढ़ता जा रहा था और इस बोलचाल की भाषा में अरबी-फ़ारसी के बहुत से शब्द इस्तेमाल होने लगे थे, इसलिए आपसी संपर्क के कारण स्थानीय भाषा में भी अरबी-फ़ारसी शब्द आ गये थे। धीरे-धीरे दो तरह की संपर्क भाषा का विकास हुआ। एक रियासत के स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा (यानी मारवाड़ में मारवाड़ी) का ही व्यवहार होता रहा लेकिन विभिन्न रियासतों और दूसरे राज्यों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में और सेनाओं में संपर्क भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा जिसे हिन्दवी, हिंदी, उर्दू आदि कहा जाने लगा था और इसका लगातार विस्तार होता गया।
मेरे परदादा के पिता और दादा हिंदी और मारवाड़ी के अलावा कोई अन्य भाषा जानते थे या नहीं, इसका प्रमाण हमारे परिवार के पास नहीं है। परदादा जिनका जन्म 1873 में हुआ था, वे मेट्रिक पास थे और उन्हें अंग्रेजी आती थी। वे जोधपुर रेलवे (आज़ादी से पहले जोधपुर रियासत द्वारा शुरू की गयी रेल सेवा जो जोधपुर से कराची तक जाती थी) में नौकरी करते थे। उनके अधिकारी अंग्रेज थे और कामकाज सारा अंग्रेजी में होता था। मेरे दादा भी मेट्रिक पास थे और उन्होंने भी अपने केरियर की शुरुआत रेलवे में नौकरी से की थी। लेकिन अपने एक दोस्त की शादी में जाने के लिए छुट्टी माँगने पर अंग्रेज अफ़सर द्वारा छुट्टी न दिये जाने पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने व्यवसाय के रूप में रेलवे से माल मँगाने और भेजने वालों की तरफ़ से रेलवे से अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करने का काम अपना लिया था। एक तरह से व्यापारी वर्ग की तरफ़ से मुक़दमा लड़ते थे और शायद इसी वजह से उन्हें वकील साहब कहकर संबोधित किया जाता था। लेकिन इस काम के लिए उन्होंने सरकार से सनद ले रखी थी। लेकिन ये सनद केवल रेलवे से पत्र-व्यवहार के लिए ही मान्य थी। पिता भी दसवीं पास थे। अंग्रेजी उन्हें भी आती थी लेकिन वे प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे जिसकी स्थापना 1930 में परदादा ने की थी। उनके काम में अंग्रेजी का उपयोग ज़्यादा नहीं था। वे अपने भाइयों के साथ प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि उनके जीवन से अंग्रेजी अनुपस्थित थी। लेकिन मेरी परदादी, दादी, बुआ और माँ सभी निरक्षर थीं। ये सब केवल मारवाड़ी में बातचीत कर सकती थीं। हाँ, चाचियों और मौसियों ने स्कूली शिक्षा हासिल की, लेकिन कोई भी मिडिल से आगे नहीं जा सकी। लेकिन मेरी पीढ़ी से लड़कियों (यानी मेरी बहनों) का न केवल स्कूल जाना शुरू हो गया बल्कि उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की। वजह यह थी कि पहले लड़कियों की शादी 15-16 की उम्र तक हो जाती थी, अब वह उम्र 20 को पार करने लगी और 24-25 तक जाने लगी। इसलिए स्वाभाविक था कि वे बी ए और एम ए तक पढ़ सकती थीं। लेकिन पढ़ने का मक़सद नौकरी करना नहीं था। इसलिए क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, इस पर न पढ़ने वाली लड़की विचार करती थी और न ही उसके माता-पिता। चूँकि लड़कियाँ पढ़ी-लिखी होती थीं, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर छोटी-मोटी नौकरी भी कर लेती थीं।
परदादा, दादा और पिता के समय शिक्षा का माध्यम हिंदी था, उर्दू नहीं, क्योंकि मेरे परदादा, दादा कोई भी उर्दू नहीं जानता था। लेकिन वे नागरी लिपि से परिचित थे। ऐसा संभवतः इसलिए था कि मारवाड़ रियासत पर कभी भी, जैसा लिख चुका हूँ, मुग़लों का शासन नहीं रहा। लेकिन राजस्थान की ज़्यादातर रियासतों के दिल्ली से अच्छे सम्बन्ध थे। दिल्ली दरबार में उन्हें ऊँचे ओहदे मिले हुए थे और उनके शासन में आमतौर पर दिल्ली की ओर से दख़लंदाजी नहीं होती थी। दिल्ली के शासकों की भाषा फ़ारसी थी। स्पष्ट है कि दिल्ली से पत्र-व्यवहार फ़ारसी में होता रहा होगा जिसके लिए फ़ारसी जानने वाले कुछ लोगों की नियुक्ति से काम चल जाता था। स्थानीय राजकाज और आम व्यवहार पहले जैसे चल रहा था, उसमें बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि उर्दू बिलकुल अनुपस्थित थी। मारवाड़ में मुस्लिम आबादी ठीक-ठाक थी और धार्मिक शिक्षा के लिए अरबी सीखने की कोशिश की जाती थी। इसी कोशिश में कुछ उर्दू भी सीख लेते थे। लेकिन उनके अपने घर की बोलचाल की भाषा मारवाड़ी थी। धार्मिक कारणों से अरबी और फ़ारसी के शब्द ज़रूर आ गये थे। लेकिन कुल मिलाकर टोंक और अजमेर जैसे इलाक़ों को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों में उर्दू हाशिये पर ही बनी रही।
शिक्षा प्रदान करने की जो व्यापक और सार्वभौम अधिरचना अंग्रेजी शासन के दौरान स्थापित और विकसित हुई, उसकी कोई ज़रूरत मध्ययुग में नहीं थी। सब अपने-अपने काम-धंधों में लगे हुए थे और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसी काम को करते जाते थे। उसका शिक्षण और प्रशिक्षण उसी स्तर पर उन्हें प्राप्त होता था। ऐसा अपवाद रूप में भी शायद नहीं होता था कि लोहार या किसान या मज़दूर का बेटा राजकाज का प्रशिक्षण लेकर राजदरबार में किसी बड़े पद पर पहुँच जाता होगा। यह बहुत महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि मध्ययुग में पश्चिम एशिया से आने वाली विभिन्न जातियाँ जिनका धर्म ज़्यादातर इस्लाम था, उनकी सामाजिक व्यवस्था हिन्दुओं से अलग थी। मुसलमानों में जातिप्रथा नहीं थी, विधवा स्त्री दुबारा विवाह कर सकती थी। लेकिन मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्था का असर हिन्दुओं पर नहीं पड़ा। धार्मिक और दार्शनिक स्तर पर ज़रूर दिखायी देता है। सामाजिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आने की वजह से ही मुग़लों के समय भी जातिप्रथा बरकरार रही। जो दलित और अछूत समझी जाने वाली जातियाँ थीं, मुस्लिम शासकों के काल में भी उनकी सामाजिक स्थिति वही बनी रही। पंडित पंडित रहा, लोहार लोहार ही रहा और दलित दलित ही। इस्लाम में धार्मिक स्तर पर कोई स्तरीकरण नहीं था लेकिन उच्च जाति के हिन्दुओं के संपर्क में आने के कारण मुसलमानों में भी कुछ हद तक सामाजिक स्तरीकरण बनने लगा जो बिलकुल हिन्दुओं की जातिप्रथा जैसा नहीं था लेकिन कुछ-कुछ उसका प्रभाव दिखायी देता था और अब भी दिखायी देता है।
मध्ययुग में देशी रियासतों का जो भी कामकाज था, वह स्थानीय भाषाओँ में पहले की भाँति चलता रहा। वह बहुत कुछ विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। दिल्ली के शासक को इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था कि अलग-अलग रियासतों के शासक कैसे शासन चलाते हैं। उन्हें सिर्फ़ दो चीज़ों से मतलब था, कर वसूलना और युद्ध के समय उस रियासत की सेना का सहयोग प्राप्त करना। लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों और अलग-अलग रियासतों के सैनिकों की भाषा अलग-अलग होती थी। उनके कमांडर फ़ारसी या तुर्की जानने वाले होते थे। इन सबके बीच संवाद ने एक नयी भाषा को जन्म दिया जो दिल्ली के आसपास की भाषा थी यानी खड़ी बोली, लेकिन उसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की के शब्द भी मिलते चले गये। यही नहीं, पत्र-व्यवहार के लिए जब उसका इस्तेमाल होने लगा तो फ़ारसी लिपि का इस्तेमाल किया जाने लगा। चूँकि भाषा हिंदुस्तान की ही थी, इसलिए इस आपसी संपर्क और संवाद की भाषा को हिंदवी कहा गया जो बाद में उर्दू के रूप में जानी गयी। इसी हिंदी या उर्दू का इस्तेमाल उन व्यापारियों द्वारा भी होता था जिन्हें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश व्यापार के सिलसिले में आना-जाना होता था। माल भेजना होता था, मँगाना होता था। इस तरह खड़ी बोली से बनी भाषा जिसे हिंदी, उर्दू, रेख्ता आदि कई नामों से जाना जाता था, पूरे उत्तर भारत की संपर्क भाषा बन चुकी थी।
संपर्क भाषा के रूप में उपयोग होने के बावजूद बोलचाल की खड़ी बोली काफ़ी समय तक काव्य की भाषा नहीं बनी क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के अलग-अलग भागों में डिंगल (राजस्थानी का एक रूप), अवधी, ब्रज, मैथिली काव्य की भाषाओँ के रूप में प्रयुक्त हो रही थीं। इनमें भी काव्य की भाषा के रूप में ब्रज का वर्चस्व ज़्यादा लम्बे समय तक और ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बना रहा। लेकिन वे कवि जो फ़ारसी पृष्ठभूमि से आये थे, वे फारसी के साथ-साथ उस भाषा में भी कविता लिखने लगे जो बोलचाल की भाषा के रूप में पूरे उत्तर भारत में प्रचलित थी और जिसे पहले हिंदवी कहते थे और बाद में उर्दू कहा जाने लगा लेकिन जिसकी लिपि फ़ारसी थी। इस भाषा में जब शायरी की जा रही थी, ठीक उस समय ब्रज में भी कविता की जा रही थी। भक्तिकाल और रीतिकाल का पूरा समय ब्रज कविता का स्वर्ण काल था। लेकिन हिंदी/उर्दू की उभरती शायरी नयी संवेदना, नयी भाषा और नये शिल्प के साथ धीरे-धीरे अपनी जगह बना रही थी। उत्तर भारत में ब्रज में कविता करने वाले भी फ़ारसी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी/उर्दू से परिचित थे हालाँकि वे स्वयं नागरी लिपि में लिखी जाने वाली ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे। नागरी लिपि में इस नयी भाषा यानी हिन्दवी को लिखना कोई मुश्किल नहीं था और उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। लेकिन कविता के बजाय गद्य के लिए उन्हें यह भाषा ज़्यादा उपयुक्त लगी जो उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू से ही पत्र-पत्रिकाओं में इस्तेमाल होने लगी थी। फ़ारसी में लिखी जाने वाली हिंदी/उर्दू में गद्य लेखन पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन फारसी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी/उर्दू में फ़ारसी/अरबी के शब्द ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे क्योंकि जिस कविता की भाषा से परिचित थे और साथ ही साथ फ़ारसी में भी लिखते-पढ़ते थे, इसलिए उसमें फ़ारसी/अरबी के ज़्यादा शब्द इस्तेमाल होते थे। इस तरह आरम्भ में जाने-अनजाने एक ही भाषा लिपि और शब्दावली (और कविता में शिल्प) के अंतर के कारण दो अलग-अलग रूपों में सामने आयी। इसे आरम्भ में हिंदवी ही कहा गया, भले ही उसकी लिपि फ़ारसी ही क्यों न हो। गद्य और पद्य दोनों में पहले शुरुआत होने के कारण फ़ारसी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी धीरे-धीरे उर्दू के रूप में जानी जाने लगी और उर्दू नाम इसका रूढ़ हो गया और वह साहित्य की रचनात्मक भाषा के रूप में स्वीकृत भी हो गयी क्योंकि मीर तकी मीर, सौदा, नज़ीर, ग़ालिब जैसे बड़े शायर उन्नीसवीं सदी के मध्य तक प्रतिष्ठित हो चुके थे जबकि नागरी लिपि में लिखी जाने वाली ब्रज अपनी चमक खोती जा रही थी। वह संवेदना और शिल्प, दोनों दृष्टियों से पुरानी पड़ चुकी थी जबकि नागरी लिपि में लिखी जाने वाली (खड़ी बोली) हिंदी अभी अपने निर्माण की पहली सीढ़ी पर थी और भाषा, संवेदना और शिल्प सभी दृष्टियों से अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी कर रही थी।
नागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी के लिए सबसे ज़रूरी था अपने को उस भाषा से अलग करना जिसे अब तक हिन्दवी या हिंदी ही कहा जा रहा था, लेकिन अब जिसके लिए उर्दू शब्द रूढ़ हो गया था। अपनी अलग पहचान की शुरुआत नागरी लिपि अपनाने से हो चुकी थी। दो लिपियों में लिखी जाकर भी (खड़ी बोली) हिंदी/उर्दू एक ही भाषा के रूप में अपनी पहचान बनाये रख सकती थीं। लेकिन नागरी लिपि में लिखनेवालों ने अरबी और फ़ारसी के शब्दों को हटाकर संस्कृत के तत्सम शब्दों को अपनाना शुरू कर दिया। अरबी और फ़ारसी के साथ कुछ हद तक देशज शब्दों की जगह भी तत्सम रूपों को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक यही कोशिश उर्दू के साथ भी हुई। अपनी अलग पहचान के लिए खड़ी बोली को फ़ारसी लिपि में लिखने वालों ने संस्कृत और देशज परम्पराओं से आये शब्दों को हटाना शुरू कर दिया। इस तरह एक ही भाषा अब दो रूपों में इस्तेमाल होने लगी और धीरे-धीरे उन्हें दो स्वतंत्र भाषाओँ के रूप में स्वीकृति भी मिल गयी। दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि इन दोनों का एक सांप्रदायिक पहलू उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन पर हावी होने लगा। फ़ारसी लिपि में लिखी जाने के कारण और अरबी-फारसी के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किये जाने के कारण सांप्रदायिक नज़रिया रखनेवाले मध्यवर्गीय हिन्दुओं ने उर्दू को विदेशी भाषा कहना शुरू कर दिया और इन्हीं लोगों ने नागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अधिकाधिक संस्कृत के नज़दीक लाने की कोशिश की और उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाने लगा।
औपनिवेशिक दौर में भाषाएँ
देशी रियासतों वाले क्षेत्र जिसे अंग्रेजों के ज़माने में राजपुताना कहा जाता था, आज़ादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के समय उसे राजस्थान नाम दिया गया। इस क्षेत्र की साहित्य की भाषा ग्यारहवीं सदी से डिंगल थी जो 16-17वीं सदी तक किसी न किसी रूप में वीरगाथा काव्य और शृंगार काव्य के लिए इस्तेमाल होती रही। लेकिन 14 सदी के उत्तरार्ध से भक्ति काव्य के लिए अवधी, ब्रज और मैथिली का उपयोग होने लगा। सूफी और रामकाव्य जो अधिकतर प्रबंध काव्य थे, अवधी में लिखे गये। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत हो या तुलसीदास का रामचरित मानस, दोनों अवधी में लिखे गये थे। लेकिन कृष्ण और शृंगार काव्य ज़्यादातर ब्रज में लिखे गये और यह परम्परा 19वीं सदी के मध्य तक जारी रही। लेकिन काव्य रचना का क्षेत्र वर्तमान राजस्थान से बिहार तक फैला था। यही वह क्षेत्र है जिसे आज हम हिंदी-उर्दू क्षेत्र के नाम से जानते हैं–उन इलाक़ों को छोड़कर जहाँ राजपूत राजाओं का शासन था। वहां फ़ारसी राजकाज की भाषा न होने के कारण उर्दू का प्रवेश भी नहीं हुआ। लेकिन खड़ी बोली का वह रूप जो अब बोलचाल की भाषा के रूप में प्रचलन में आ चुका था और जिसे हिन्दवी, हिंदी, रेख्ता, उर्दू के नाम से पहचाना जाने लगा था, राजपुताने से लेकर बिहार तक बोला और समझा जाता था। जब इस बोलचाल की भाषा को लिखने की ज़रूरत हुई, तब यह पहले फ़ारसी लिपि में लिखी जाने लगी और बाद में नागरी लिपि में भी लिखी जाने लगी। लिखने की ज़रूरत इसलिए हुई कि अंग्रेजों के आगमन के बाद प्रिंटिंग प्रेस का आगमन भी हुआ और कई भाषाओँ में अखबार और पत्रिकाएँ निकलने लगीं। उर्दू में पहला अखबार ‘जमे जहाँ नुमा’ 1822 में और हिंदी समाचार पत्र ‘उदन्त मार्तंड’ 1826 में प्रकाशित हुए। राजा राममोहन राय (1772-1833) ने फ़ारसी, बांग्ला और हिंदी में भी पत्र निकाले।
मध्ययुग में राजकाज के बहुत छोटे स्तर पर फारसी का उपयोग होता रहा हो, बिलकुल वैसे ही जैसे अंग्रेजों के समय अंग्रेजी का होता था। इसलिए शिक्षा में कोई बड़ा बदलाव मध्ययुग में नहीं हुआ। मध्ययुग में सवर्णों को छोड़ कर शेष जातियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने सामाजिक वर्ग नहीं बदल सकती थीं क्योंकि उनके लिए शिक्षा की कोई सार्वभौम व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने शिक्षा और सरकारी कामकाज का जो ढाँचा स्थापित किया, वह सार्वभौम था और उसके दरवाज़े सभी के लिए खुले थे। उनमें सवर्ण और अवर्ण, पुरुष और स्त्री और हिन्दू और मुसलमान सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। यह काम बहुत आसान नहीं था। जातिवाद इस सार्वभौम शिक्षा के विस्तार में सबसे बड़ा अवरोध था। यहाँ इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ इतना कहना पर्याप्त है कि भाषा का मसला मध्ययुग में इतने बड़े स्तर पर नहीं देखा गया था जो अंग्रेजों के शासन के समय देखे जाने की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि उन्होंने एक मध्ययुगीन शासन व्यवस्था को आधुनिक शासन व्यवस्था में बदलने की कोशिश की और इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण और आधुनिकीकरण की थी। यह सही है कि अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम बनाकर अंग्रेजी को फ़ारसी की तुलना में कहीं ज़्यादा विस्तार दिया। फ़ारसी केवल मुसलमानों और हिन्दुओं के अभिजात वर्ग तक ही सीमित रही और वहाँ से भी धीरे-धीरे लुप्त होने लगी। लेकिन अंग्रेजी उन सब लोगों तक पहुँची जो शिक्षा के आधुनिक संस्थानों तक अपनी पहुँच बना सके। इस अंग्रेजी शिक्षा ने एक नया मध्यवर्ग पैदा किया जो मध्ययुगीन अभिजात वर्ग से कहीं ज़्यादा बड़ा था। वे अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से सिर्फ़ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हासिल नहीं कर रहे थे, ज्ञान-विज्ञान के नये क्षेत्रों का ज्ञान और कौशल भी हासिल कर रहे थे जिसका विकास पश्चिम के देशों में हुआ था। इसी मध्यवर्ग से ऐसा शिक्षित समुदाय भी सामने आ रहा था जो पश्चिम की दुनिया में वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर होने वाले बदलावों से प्रभावित और प्रेरित होकर इस बात को महसूस कर रहे थे कि अंग्रेजों ने हमें वे अधिकार नहीं दिये हैं जो उन्होंने अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिये हैं। इसमें सबसे बड़ा अधिकार अपने जनप्रतिनिधि चुनना था जो एक निश्चित अवधि के लिए शासन चलाते थे। अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार भारतीयों को नहीं था। धीरे-धीरे उन्हें यह अहसास भी हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे देश को उपनिवेश बना लिया है और हमें अपना ग़ुलाम। इस गुलामी से मुक्ति आवश्यक है। गुलामी का बोध और उससे मुक्ति की इच्छा का ज्ञान भी काफ़ी हद तक भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा की ही देन था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों में गुलामी और उससे मुक्ति का अहसास तीव्र होने लगा, तब अंग्रेजी एक औपनिवेशिक भाषा के रूप में हमारे ऊपर लादी जाने के बावजूद अब वह औपनिवेशिक भाषा नहीं रही थी। वह उन सब भाषाओँ की तरह भारतीय भाषा बन चुकी थी जो हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम थी। उर्दू तो इसलिए और ज़्यादा हमारे नज़दीक थी कि उसका जन्म ही भारतीय भाषा से हुआ था, भले ही वह एक विदेशी लिपि में लिखी जाती हो और उसमें विदेशी शब्द बहुत अधिक हों।
मारवाड़ का व्यापारी वर्ग मुग़लों के समय से ही बाहर जाने लगा था। रेगिस्तानी इलाक़ा होने के कारण अकाल पड़ना, पानी की कमी होना, बहुत कम फसलों का होना आम बात थी। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हमारा परिवार जो जोधपुर के पास एक गाँव में आढ़त का काम करता था, गाँव छोड़ कर शहर में आ बसा था। 1900 ईस्वी में जो भयंकर अकाल पड़ा और प्लेग फैला, उसमें राजपुताने (राजस्थान का पुराना नाम) की लगभग एक तिहाई आबादी की मौत हो गयी थी। खेती उजड़ गयी, व्यापार उजड़ गया। राजस्थान छोड़कर बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजस्थान की पैदाइश के बल पर व्यापार की गुंजाइश कम थी। इसलिए ऐसे प्रदेशों में जाकर व्यापार करना ज़्यादा लाभप्रद था जहाँ पैदावार भी ज़्यादा होती थी और कुछ ऐसी चीज़ें निर्मित होती थीं जिनका देश-विदेश में व्यापार फ़ायदेमंद था। हमारे ही परिवार की एक शाखा 1910 के आसपास पहले महाराष्ट्र और बाद में गुजरात के वापी क्षेत्र में जा बसी थी।
मुग़लों के ज़माने में पैदावार और निर्माण के क्षेत्र का विस्तार होने से व्यापार का भी विस्तार हुआ और इस वजह से राजपुताने के व्यापारी अपने काम-धंधे का विस्तार कर सके। अंग्रेजों के समय भी यह प्रक्रिया चलती रही। हालाँकि अंग्रेजों ने कई भारतीय उत्पादों को नुकसान पहुँचाया जब वे चीज़ें निर्यात होने की बजाय इंगलैंड और यूरोप से उनका आयात होने लगा। उदहारण के लिए जो कपड़े हाथकरघा से बनते थे और भारत से निर्यात किये जाते थे, अब इंगलैंड और यूरोप में पॉवरलूम यानी बिजली से चलने वाले करघे से बनने लगे। ये कपड़े हाथकरघा से बनने वाले कपड़े से जल्दी बनते थे, सस्ते और बेहतर होते थे। यानी जो कपड़ा पहले भारत से बाहर जाता था, अब उसका भारत में आयात होने लगा। लेकिन इस दौर में कई नये तरह के उत्पादों की शुरुआत भी हुई और मारवाड़ी व्यापारियों का व्यापार बीच-बीच में कुछ धक्के खाते हुए चलता रहा और बढ़ता रहा। इसके साथ ही राजस्थान के व्यापारी व्यापार के सिलसिले में देश के हर हिस्से में पहुँच गये और इसके साथ ही बोलचाल की हिंदी भी पहुँच गयी।
ऐसा नहीं है कि राजस्थान के व्यापारी ही सारे देश में फैले। दूसरे प्रदेशों से भी लोग अन्य प्रदेशों में गये। शासन-प्रशासन की जिस नयी व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों के समय हुई, उसमें अग्रेज़ी शिक्षा का बड़ा महत्त्व था। अठारहवीं सदी से जिस आधुनिक शिक्षा का विस्तार हुआ, उसके साथ अंग्रेजी जानने वाले मध्यवर्ग का उदय भी हुआ जो शासन-प्रशासन और अध्यापन के काम को करने में प्रशिक्षित थे। अपने अंग्रेजी ज्ञान के बल पर वे दूसरे प्रदेशों में जाकर भी नौकरी करने में सक्षम थे और वे गये भी। लेकिन केवल अंग्रेजी से वे स्थानीय लोगों से संवाद नहीं कर सकते थे। यह संवाद संभव हुआ उस हिन्दवी के बल पर जो सोलहवीं-सत्रहवीं सदी में ही संपर्क भाषा बन चुकी थी, भले ही वे उसे बहुत अच्छे ढंग से न बोल सकते हों, लेकिन सुनकर समझने वे लगे थे। जो अच्छे से पढ़ और लिख सकते थे, वे भले ही उसे फारसी लिपि (यानी उर्दू) या नागरी लिपि (यानी हिंदी) में लिखते हों, लेकिन वह हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से की संपर्क भाषा बन चुकी थी। सिनेमा की शुरुआत से बहुत पहले।
आज़ादी के बाद का भारत
यही वजह है कि व्यापार या मेहनत मज़दूरी के लिए अपने प्रदेशों से बाहर जानेवालों के लिए किसी और भाषा में शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं थी। राजपुताने के व्यापारी जहाँ भी व्यापार करने गये, वे उस संपर्क भाषा से परिचित थे जिन्हें हिंदी, उर्दू, हिन्दुस्तानी कई नामों से जाना जाता था। ये दो सौ साल पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है। कुछ समय बाद ही उन्हें वहाँ बोलचाल लायक भाषा सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। जैसा कह चुका हूँ, पश्चिम से पूर्व तक खड़ी बोली बाज़ार की संपर्क भाषा बन चुकी थी। इस तरह बोलचाल की भाषा खड़ी बोली के साथ वे उन प्रदेशों में व्यापार करने लगे। अन्य व्यापारियों और स्थानीय खरीददारों से तो वे बोलचाल की खड़ी बोली में संवाद करके अपना काम चला लेते थे, लेकिन नवाबों और अभिजात परिवारों के लिए शुरू में दुभाषियों की मदद लेते रहे होंगे। लेकिन धीरे-धीरे एक-दो पीढ़ी बाद ही फ़ारसी, बांग्ला और दूसरी भारतीय भाषाएँ जाननेवाले स्वयं उनके परिवारों में पैदा हो चुके थे। उसकी वजह यह थी कि उनके बाद की पीढ़ी जो उनके साथ वहीँ रहती थी, वहाँ की स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करने लगी थी। वे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हुए भी एक विषय के रूप में वहाँ की स्थानीय भाषा (मसलन बंगला, ओडिया, असमी, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि) भी सीखते थे। वे बच्चे जो वहीँ पल-बढ़ रहे थे, स्कूल, आस-पड़ोस और बाज़ार के ज़रिये वहाँ की स्थानीय भाषा को मातृभाषा की तरह ग्रहण कर रहे थे। इस संवाद और संपर्क के माध्यम से वे स्थानीय भाषा को अपनी मूल मातृभाषा से ज़्यादा बेहतर बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाते थे। कइयों ने तो स्थानीय भाषा को मातृभाषा की तरह अपना लिया था। असमी के बड़े लेखक ज्योतिप्रसाद अगरवाला राजस्थान के रहने वाले थे। शिवप्रसाद सितारेहिंद जो मूलरूप में राजस्थान के रहने वाले थे, उनके पूर्वज राजस्थान से निकलकर मुर्शिदाबाद में जाकर मुगलों के समय में ही बस गये थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्वज भी राजस्थान से ही जाकर बंगाल में बसे थे और बाद में बनारस आ गये थे। मेरी ममेरी बहनें जो चेन्नई में रहती थीं, तमिल धाराप्रवाह बोल सकती थीं। उत्तर भारत के बहुत से राज्यों में पंजाब, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों से आकर लोग बसते रहे हैं और उनके लिए हिंदी ठीक वैसी ही होती है जैसी हिंदीभाषियों के लिए। हिंदी और उर्दू के कई साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी (या इन कथित हिंदी प्रदेशों की अपनी भाषाएँ जैसे राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी) नहीं थीं, उन्होंने भी हिंदी को मातृभाषा की तरह न केवल अपना लिया है बल्कि उसे अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनाया है। गजानन माधव मुक्तिबोध की मातृभाषा मराठी थी लेकिन वे हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हीं के सगे भाई शरतचंद्र मुक्तिबोध मराठी के साहित्यकार थे। पंजाबी मातृभाषा के बहुत से लेखक उर्दू या हिंदी के लेखक रहे हैं। इसी तरह बंगाली मातृभाषा के बहुत से लेखक हिंदी के लेखक हैं। सुदीप बनर्जी, प्रणव कुमार बंद्योपाध्याय हिंदी लेखक थे। कहने का अर्थ सिर्फ़ इतना है कि मातृभाषा कोई ऐसी स्थायी चीज़ नहीं है जो बदलती न हो। व्यापक संपर्क और संवाद की भाषा मातृभाषा बने, यह भी आवश्यक नहीं है। उसमें जिस भाषा में हमने शिक्षा ली है, उसकी भूमिका मातृभाषा से ज़्यादा व्यापक हो सकती है। यही नहीं, एक ही समय में हम अलग-अलग परिवेशों और अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग भाषाओँ का इस्तेमाल करते हैं। मसलन, मेरे परिवार के लिए घर की भाषा अलग (मसलन, मारवाड़ी और हिंदी), शिक्षा की भाषा अलग (हिंदी और अंग्रेजी), मनोरंजन की भाषा अलग (हिंदी और अंग्रेजी), संपर्क की भाषा अलग (हिंदी और अंग्रेजी)। यह विभाजन मेरे पर लागू होता है क्योंकि मैं गुडगाँव में रहता हूँ। लेकिन मेरे बच्चों पर नहीं। उनके यहाँ मारवाड़ी पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। शिक्षा की भाषा अंग्रेजी है और मनोरंजन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। दिल्ली-गुड़गाँव में ही रहनेवाले किसी बंगाली, मराठी या मलयाली के यहाँ हिंदी और अंग्रेजी तो होगी और उनकी मूल मातृभाषा भी एक-दो पीढ़ियों तक बनी रहेगी। लेकिन बहुत मुमकिन है कि अगर वे अपने परिवार में अपने माता-पिता या दादा-दादी की भाषा को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह एक दिन लुप्त हो जायेगी। लेकिन कुछ भाषाएँ जीवन में ऐसी जगह बना लेती हैं कि वे कई पीढ़ियों तक बची रहती है। उदहारण के लिए, हिंदी सिनेमा (जिसे हिन्दुस्तानी सिनेमा कहना ज़्यादा उपयुक्त है) की भाषा लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में समझी जाती है, भले ही बहुत बड़ी आबादी न नागरी लिपि जानती हो और न ही उर्दू लिपि। हिंदी और उर्दू कभी उनकी मातृभाषा भी न रही हो और न शिक्षा की भाषा रही हो और काफ़ी हद तक उनकी संपर्क भाषा भी न हो, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप जिस व्यापक और मिलीजुली सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण सिनेमा और टेलीविज़न ने उन्हें न केवल हिन्दुस्तानी से जोड़ रखा है बल्कि वे उसे समझने की क्षमता भी रखते हैं। हालाँकि आजकल जिस तरह की हिंदुत्वपरस्त प्रचार फ़िल्में बन रही हैं, वे इस मिलीजुली सांस्कृतिक परंपरा के विरोध में जाती हैं और तब हिंदी सिनेमा की व्यापक लोकप्रियता और स्वीकृति को बनाये रखना भी मुश्किल होगा।
हमारे जीवन में एक साथ एक से ज़्यादा भाषाओँ की उपस्थिति बदलाव की स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि आज से सदियों पहले जब हम एक ही गाँव, एक ही शहर में और एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार में रहते थे, वह जीवन, वह परिवेश अब पीछे छूट चुका है। यह कहना तो तब भी सही नहीं था कि बदलाव की यह प्रक्रिया पूरी तरह ग़ैरहाज़िर थी, बहुत सारी चीज़ों के साथ भाषा भी बदलती थी, लेकिन आज जिस तरह विस्थापन रोज़मर्रा के जीवन का अंग बन गया है, उस तरह और उस पैमाने पर शायद तब नहीं था। पहले भी लोग अपना गाँव, अपना देश छोड़कर दूर-दूर जाते थे और वहाँ बस जाते थे। आमतौर पर इसके पीछे प्राकृतिक कारण होते थे। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी महामारी। और कभी-कभी किसी निर्दयी हमलावर की बड़े पैमाने पर लूटपाट और नरसंहार। लेकिन तब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आम आदमी को न पासपोर्ट की ज़रूरत होती थी और न ही वीजा की। जिसे आज हम राष्ट्र यानी नेशन कहते हैं, वैसी कोई संकल्पना तब नहीं थी। खेती ने लोगों को जीवन में ज़्यादा स्थिरता दी थी। व्यापार काफ़ी हद तक पैदावार से जुड़ा था, इसलिए स्थायित्व के लिए भी इधर-उधर भटकने के बजाय एक जगह से व्यापार करना ज़्यादा मुफ़ीद था। लेकिन अब नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अपने गाँव, अपने देश को छोड़कर बिलकुल अनजाने और अपरिचित प्रदेशों में जाना होता है। यह बात मेहनतकश ग़रीबों पर भी लागू होती है, शिक्षित मध्यवर्ग पर भी लागू होती है और अमीर अभिजात और पूँजीपतियों पर भी लागू होती है। दिल्ली और गुडगाँव में मेहनत-मज़दूरी करनेवाला बंगाली और ओड़िया भाषी का टूटी-फूटी हिंदी से काम चल जाता है। बिहार से पंजाब जाकर खेतों में काम करनेवाले से पंजाबी किसान हिंदी से काम चलाता है। लेकिन एक शिक्षित बंगाली या तमिल भाषी जब दिल्ली आता है तो जिस कंपनी और संस्थान में वह काम करता है, वहाँ अंग्रेजी उसकी मददगार होती है। लेकिन घर में काम करनेवाली नौकरानी का काम के समय और बाज़ार में खरीदारी करते वक़्त टूटी-फूटी हिंदी से काम चल जाता है। हो सकता है, इस हिंदी के लिए फ़िल्म और टेलीविज़न पर इस्तेमाल होने वाली हिंदी मददगार हो। अब तक के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मौजूदा भारत में केवल एक भाषा को जानना पर्याप्त नहीं है। तब और भी मुश्किल है जब पूरी दुनिया और दुनिया के लगभग सभी देश अतीत के किसी भी काल-खंड की तुलना में आज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। सम्प्रेषण के संसाधन इतने तीव्र और व्यापक हो गये हैं कि उनके बीच संवाद और संपर्क आसान हो गया है।
इस मौजूदा दुनिया में भारत जैसा बहुभाषी देश किसी एक भाषा से सब काम नहीं ले सकता। भारत जैसे देश को दो स्तरों पर संपर्क भाषा की ज़रूरत होती है। एक, पूरे देश के पैमाने पर ताकि अलग-अलग प्रान्त के लोग उस संपर्क भाषा के माध्यम से आपस में संवाद कर सकें। अब तक हिंदी, उर्दू और हिन्दुस्तानी से काफ़ी हद तक काम चलता रहा है। दूसरी संपर्क भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी अन्य देशों से संपर्क करने के लिए। हम इस बात को पसंद करें या न करें, लेकिन अपने अनुभव से जानता हूँ कि अंग्रेजी ही अकेली ऐसी भाषा है जिसके सहारे आप ज़्यादातर देश घूम सकते हैं और वहाँ के लोगों से संवाद भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ बस भी सकते हैं। मातृभाषा की तरह संपर्क भाषा को विधिवत सीखने की आवश्यकता नहीं होती। व्यवहार में अधिकाधिक उपयोग से ही संपर्क भाषा सीखी भी जाती है और उसमें अधिकाधिक प्रवीणता भी हासिल होती जाती है। जिस तरह मातृभाषा को थोपने की ज़रूरत नहीं होती, उसी तरह संपर्क भाषा को भी अन्य भाषा-भाषियों पर थोपा नहीं जाना चाहिए।
चीन, जापान, रूस आदि विकसित देश जो अंग्रेजी का कम और अपने देश की भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन्होंने उच्च शिक्षा में उपलब्ध उस नवीनतम ज्ञान को जो उनकी भाषा में नहीं है, अपने देश की भाषा में तत्काल उपलब्ध कराने का अनुवाद का व्यापक आधुनिकतम तंत्र विकसित कर रखा है। हालाँकि ये देश भी अंग्रेजी भाषा के महत्त्व को समझने लगे हैं। पेकिंग विश्वविद्यालय के एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए मैं अगस्त 2004 में चीन गया था। वहाँ आपका अंग्रेजी ज्ञान काम नहीं आता। अगर आप चीनी नहीं जानते हैं तो आपको कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की दो महिलाएँ विश्वविद्यालय के प्रवेशद्वार पर काफ़ी कोशिश के बावजूद वहाँ ड्यूटी दे रहे सुरक्षाकर्मियों को नहीं समझा पायीं कि उन्हें कहाँ जाना है। दरअसल उन्हें विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में जाना था। ठीक उसी समय मेरे मित्र राकेश वत्स और मैं वहाँ से गुज़रे। राकेश वत्स विश्वविद्यालय के परिसर में ही रहता था और अथिति अध्यापक के रूप में नियुक्त था। राकेश को चीन में रहते हुए लगभग दो साल हो गये थे और इस दौरान इतनी चीनी सीख ली थी कि वह सुनकर समझ सकता था, चीनी में जवाब दे सकता था और लिखा हुआ पढ़ सकता था। वे सुरक्षाकर्मी राकेश को जानते भी थे। उन्होंने तत्काल राकेश को रोका और उससे चीनी में पूछा कि ये महिलाएँ क्या कह रही हैं। सुरक्षाकर्मी इतना समझ गये थे कि ये महिलाएँ भी राकेश के ही देश यानी इंडिया की होंगी। विदेश में भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, (अफगानी और श्रीलंकाई भी) के बीच लोग फ़र्क़ नहीं कर पाते। उन्हें एक ही समझते हैं। इस ग़लतफ़हमी का सुखद पहलू ये है कि पाकिस्तानी, बंगलादेशी और (कुछ हद तक) हिन्दुस्तानी बड़े प्रेम से मिलते हैं और एक-दूसरे की मदद भी करते हैं। हमें देखकर वे महिलाएँ भी उत्साहित हो गयीं और हिंदी (उनके लिए उर्दू और वास्तव में हिन्दुस्तानी) में बात करने लगीं। राकेश ने उनसे बात करके सुरक्षाकर्मियों को बताया कि इन्हें गेस्ट हाउस जाना है। लेकिन मेरे दोस्त राकेश ने यह भी बताया कि चीन में अग्रेज़ी सिखाने का बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 2008 में बीजिंग में ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है और चीन की सरकार यह नहीं चाहती कि विदेशी पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। कैब चलानेवाले ड्राईवर, होटलों में काम करनेवाले वेटर और ऐसी सब जगहों पर जहाँ पर्यटक जाते हैं, वहाँ काम करनेवालों को अंग्रेजी सिखाने का अभियान चलाया जा रहा है। उनके लिए विशेष कक्षाएँ चलायी जा रही हैं। इसकी पुष्टि मेरे सामने एक कैब ड्राईवर ने की भी थी। लेकिन यह भी बताया कि चीन की स्कूलों में कुछ सालों पहले ही प्राइमरी स्तर से अंग्रेजी विषय को अनिवार्य कर दिया गया है और स्पष्ट है कि स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करने के पीछे सिर्फ़ ओलम्पिक का आयोजन नहीं था बल्कि वैश्विक स्तर पर चीन की पहुँच को विस्तार देना था और इसी का परिणाम है कि आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रति व्यक्ति आय में भी भारत से बहुत आगे है।
भारत की तुलना चीन से करना उचित नहीं है लेकिन उसके अनुभवों से सीखा ज़रूर जा सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बराबर है लेकिन अन्य कई मामलों में भारत काफ़ी अलग है। भारत बहुभाषी देश है जहाँ संविधान में 22 भाषाओँ को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है जबकि चीन में मुख्य रूप से एक ही भाषा चीनी (मंदारिन) का हर क्षेत्र में उपयोग होता रहा है जबकि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इन 22 भाषाओँ का उपयोग करना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि ग़रीब विद्यार्थियों (जिनमें ज़्यादातर दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं) के प्रतिकूल भी है। उदहारण के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक प्रबंधन, विधि, विज्ञान आदि की शिक्षा भारतीय भाषाओँ में प्रदान करने पर इसकी सम्भावना बहुत ज़्यादा है कि वे रोज़गार के क्षेत्र में पिछड़े रह सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन सभी विषयों की उत्कृष्ट पुस्तकें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं जबकि आज़ादी के 78 साल बाद भी इन विषयों में उच्चस्तरीय पुस्तकें भारतीय भाषाओँ में लगभग नहीं हैं। अगर पुस्तकें लिखी भी जाती हैं तो वे अलमारियों में ही क़ैद रह जाती हैं। इसलिए भाषा, साहित्य और मनोरंजन को छोड़कर शेष सभी विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के साथ-साथ यदि भारतीय भाषाओँ में कराया जाता है तो दो तरह के उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी होंगे और कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय भाषाओँ में अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी न केवल पिछड़ जायेंगे बल्कि उनके लिए रोज़गार प्राप्त करना भी मुश्किल होगा। इसलिए उच्च शिक्षा के स्तर पर अध्ययन-अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए ताकि क्षेत्र विशेष में पूरी दुनिया में जो ज्ञान उपलब्ध है, उसका अध्ययन करने में विद्यार्थी को किसी तरह की कठिनाई न हो। भाषा, साहित्य और मनोरंजन उस राज्य की भाषा में या जिस भाषा का अध्ययन विद्यार्थी करना चाहता है, उसका माध्यम के रूप में उपयोग करने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए।
उच्च शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी लागू करने का मतलब है साहित्य, कला और भाषा जैसे विषयों को छोड़कर शेष सभी विषय उच्च शिक्षा के स्तर पर केवल अंग्रेजी माध्यम हो। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेजी को प्रान्त की राजभाषा के साथ-साथ पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा तक पहुँचते-पहुँचते अग्रेज़ी उनके लिए उतनी ही सहज और सरल हो जितनी उनकी अपनी भाषा। ग़ैर हिंदी भाषी प्रदेशों में अगर तीसरी भाषा के रूप में हिंदी (या उर्दू) भी सिखायी जाती है तो इसका विद्यार्थियों को लाभ ही होगा। लेकिन अगर कोई राज्य हिंदी सिखाने के लिए तैयार नहीं है तो उन पर इसके लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदी प्रांतों में जहाँ प्रांतीय भाषा के रूप में हिंदी पहले से ही पढायी जाती रही है, वहाँ ग़ैर हिंदी प्रदेश की एक भाषा या अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य विदेशी भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनमें भारत और विदेश की उन क्लासिकल भाषाओँ को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो अब लोक-व्यवहार में प्रचलित नहीं है। हाँ, उच्च शिक्षा के स्तर पर इन क्लासिकल भाषाओँ के अध्ययन-अध्यापन और शोध को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी तरह वे भाषाएँ जिन्हें उपभाषा या बोली कहकर एक तरह से किनारे कर दिया गया है, इनको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विश्वविद्यालयों में विशेष विभाग और शोध और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सरकार के अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए।
हिंदी पहले से ही संपर्क भाषा के रूप में पूरे भारत में मौजूद है। बिना राजकीय दबाव के वह ज़्यादा आसानी से ग़ैर हिंदी भाषियों के द्वारा स्वीकार की जाती रही है और आगे भी की जाती रहेगी। भारतीय भाषाओँ के बीच परस्पर संवाद और आदान-प्रदान का माध्यम साहित्य, कला और मनोरंजन को बनाया जाना चाहिए। साहित्य और सिनेमा हमेशा से ही ऐसे माध्यम रहे हैं। इस तरह अन्य भारतीय भाषाओँ के साथ-साथ हिंदी भी फलती-फूलती रहेगी। बेहतर तो यह होगा कि हिंदी को पूरे देश की राजभाषा का दर्जा देने की बजाय केवल उन राज्यों की राजभाषा के रूप में ही मान्यता प्राप्त हो जहाँ की वह प्रमुख भाषा है। संपर्क भाषा के रूप में तो वह पूरे देश में वह पहले से मौजूद है ही।
jparakh@gmail.com

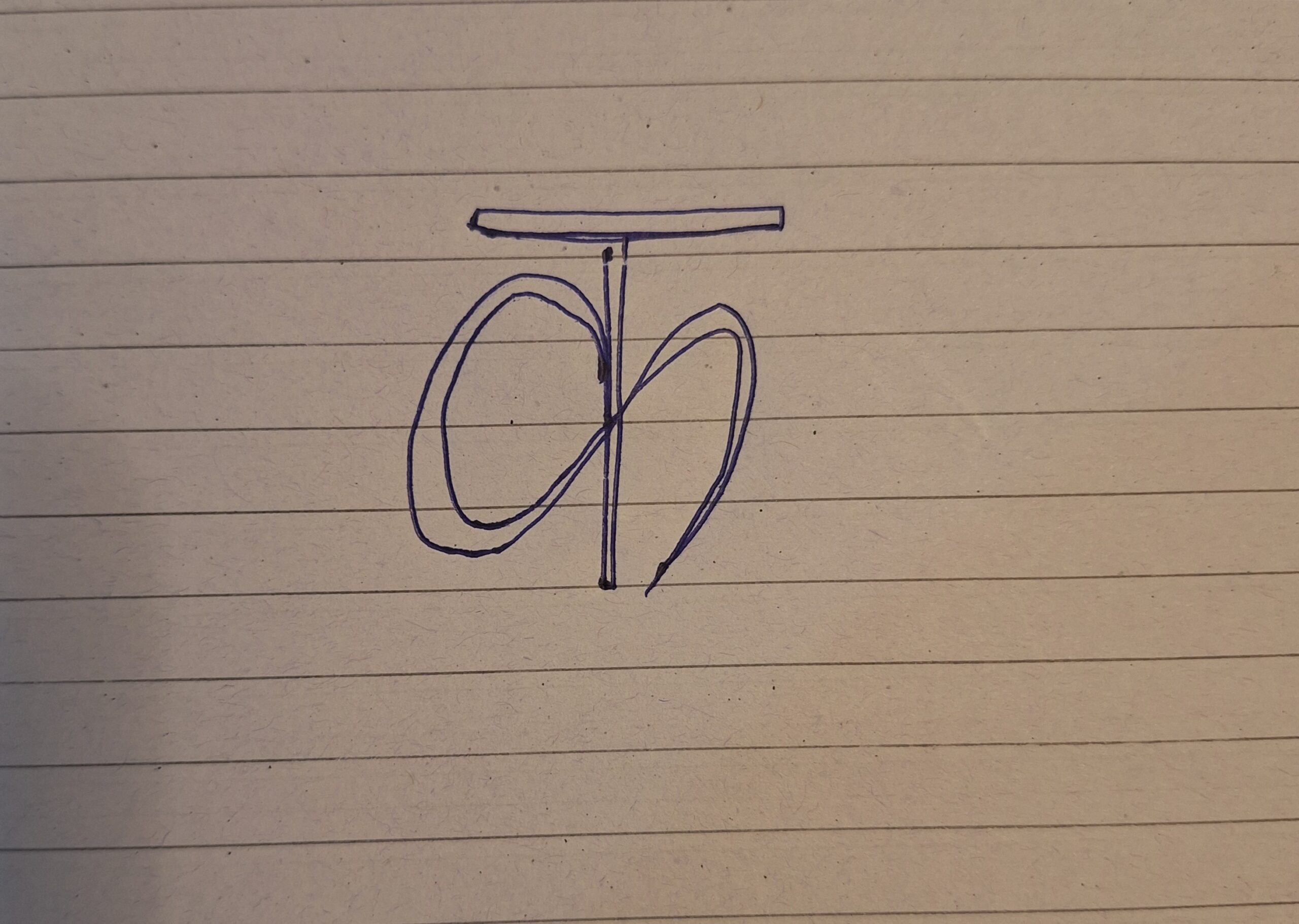







बेहद तार्किक नज़रिए से भाषा के सवालों पर ज़व्वरीमल पारख जी का आलेख महत्वपूर्ण है। इसमें मारवाड़ यानि आज के राजस्थान के जनजीवन में पिछले 200 वर्षों से भाषाओं, बोलियों से विकसित संपर्क भाषा के विकास पर आज की युवा पीढ़ी तक की भाषा की उपस्थिति का विशद उल्लेख है। बेहद व्यावहारिक रूप से पारख जी यह भी बताते हैं कि दिल्ली तथा अन्य महानगरों में उच्च शिक्षित युवा हिंदी के बराबर या अधिक अंग्रेजी का प्रयोग न केवल आम बोलचाल में बल्कि मनोरंजन के लिए फिल्म आदि देखने में करते हैं। किस प्रकार मंदारिन पर एकाग्र करने वाले चीन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहुंच और बाज़ार को ध्यान में रखते हुए अपने यहां 2004 से अंग्रेजी भाषा को पठन पाठन में शामिल करवा के आज विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफलता हासिल की।
इसके साथ ही स्थानीय बोलियों के प्रभावक्षेत्र का भी उन्होंने उसी शिद्दत से जिक्र किया, जिसके साथ साथ हिंदी को उच्चारण के स्थानीय प्रभावों से मुक्त एक भाषा के रूप में कैसे विकसित होना चाहिए़ इसके बारे में उनकी सजगता विचारणीय है।
हम सब कथित हिन्दी राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा और रायपुर अंचल, मध्यप्रदेश के मालवा, बुंदेलखंड और महाकौशल, उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड अंचलों, उत्तराखंड के गढ़वाली और तराई अंचल, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला तथा शिमला मंडी के अंचल, बिहार के मधुबनी और दरभंगा , झारखंड का छोटानागपुर पठार और रांची गढ़वा , हरियाणा के मेवात और रोहतक इलाकों के लोग भाषा की इन स्थितियों को इस आलेख के साथ एकजुट पाते हैं। मोटे तौर पर हिंदीभाषी कहे जाने के बावजूद इन अंचलों की हिंदी स्थानीयता के भारी प्रभावों से युक्त है।
भाषा के मुद्दे पर एक जरूरी आलेख
पी सी रथ
रायपुर, छत्तीसगढ़
91312 10063
बहुत बहुत धन्यवाद !
आलेख गहन विश्लेषणपरक है। इसमें पद्य की भाषा हिन्दी करने के लिए अयोध्या प्रसाद खत्री का स्मरण किया जाना चाहिए था।