‘लोकतंत्र में लोक को तिज़ोरी और पेटी में क़ैद करना किसी कला से कम नहीं है।’–प्रदीप्त प्रीत की कविताएँ :

वे लोग
सूखे-सूने और बिलबिलाते महावन में
अजीब सा दुःख गोले बरसाता है
नयी सदी का उत्थान है या मनुष्यता का पतन है
या है दब चुकी आवाज़ों का दुःख
जो मन को बार-बार नृशंस मार देता है
पूछता भी नहीं है – जाति क्या है तुम्हारी? कौन सा धर्म तुम्हें यहाँ तक जीवित रहने को पोषता है?
आसमान में फैली सिन्दूरी पताका है
या करिश्माई सम्मोहन है
जो छलछलाता रहता है महावन के जलाशयों में
जिसकी एक बूँद भी हरे-भरे पेड़ को क्षण भर में ठूँठ कर देती है
ये किस प्रजाति की वल्लरियाँ हैं
जो कंकालों को ढँकने के लिए बढ़ती रहती हैं दिन-रात
हवा और पानी नहीं तो क्या है इनका आहार
ये किसका लहू है जो इनकी नसों में फटने को आतुर है लाल-लाल
वे जो रोटी, सेहत और बरसात की दुआ करते थे
और जिनकी आँखों में समय कभी सवाल बनकर नहीं उतरा
जो बचते-बचाते रहे खुद को और खुदा को
वे जो घर जाना चाहते थे
उन घरों में
जिन्हें किसी रहस्यमयी आग ने पिघला दिया है
और जहाँ से आकर वे बीत चुके हैं
कहाँ गये वे लोग?
000
‘मुझे ग्यारह रन और बनाने हैं’
(इलाहाबाद से जाते हुए)
अभी ऊबा नहीं हूँ यहाँ से
कई परतों की तह में छुपा हुआ है इंद्रधनुष
अभी भी उतना ही नया है तुम्हारा आलिंगन
कितने अपरचित हो तुम, मेरे इलाहाबाद!
उदास चेहरों के उदास शहर, तुम्हारी कविताई की खुराक क्या है?
महज़ ग्यारह दिन और रह गये हैं मेरे पास
बसंत त्रिपाठी कह रहे हैं शेखर जोशी की याद में
एक बड़ा कार्यक्रम करना है
नौ और दस सितंबर को
सत्रह को तो मैं चला ही जाऊँगा
उसी पल सोच रहा था कि प्रणय कृष्ण से मिलना है एक पूरा दिन और उनकी बड़ी-बड़ी डबडबाई आँखों में देखना है चन्दू और गोधरा को
‘मैं इक्कीसवीं सदी का एक दृश्य हूँ’ अब तो क्या ही सुन पाऊँगा हरीश चन्द पाण्डे से, उनसे मिलना उनके रचनात्मक क्षणों में दख़ल देना नहीं होगा?
एक दिन भूत बनकर थियेटर जाना है और देखना है क्या चल रहा है वहाँ
किताबों पर जम चुकी धूल को एक आख़िरी बार हटाना है
न जाने जाने के बाद दोबारा लौटकर आने का वक़्त होगा कि भी नहीं
पूरा दिन बघाड़ा से सिविल लाइंस थाहाने के बाद एक पूरी शाम दोस्तों को देखकर कहना है एक दिन हम खुलकर हसेंगे और हाँ, कभी याद आये तो ‘चिट्ठी’ मत लिखना
आख़िरी रात तुम्हारे उदास चेहरे को सहेजना चाहता हूँ मैं, जाना नहीं चाहता हूँ
और पूछता हूँ कि जाऊँ कि न जाऊँ?
वह कौन सा डर है जो यह कहने नहीं देता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ
क्योंकि मैं कहता हूँ मुझे बहुत दूर जाना है अब, और नहीं घुटना है।
टिकट की वेटिंग लिस्ट ख़त्म होने का नोटिफिकेशन आयेगा
और मागूँगा सिगरेट जो बैंक रोड से तुम मेरे लिए लायी रहोगी।
एक आख़िरी बार मैं तुम्हें गले लगाऊँगा और बादलों में छिप जाऊँगा।
कोई एक तारा टूटेगा और समंदर में डूब मरेगा।
[शीर्षक शेखर जोशी की एक कविता की पंक्ति है।]
000
नोट
मेरी अभिव्यक्ति का स्वरूप कैसा हो?
एक निर्वात में फँस गया हूँ
स्थूल से दृश्य पिघलकर
रंगों की तरह छिटकने लगते हैं
जले हुए का निशान पीठ पर पड़ जाता है
देख रहा हूँ
मज़दूरों से खचाखच भरी हुई भागती ट्रेन
पिघलकर खेतों में कहीं गुम हो गयी
खेत सिकुड़कर बोरियों में कैद हो गये
बोरे छोटी सी तिजोरी में समा जाने की हड़बड़ी में हैं
यह महज़ एक कलात्मक दृश्य है
जिसमें बड़ी सी ट्रेन
विस्तृत खेत
लॉरियों का खेमा
एक तिजोरी में कैद हो गये
तिजोरी का जादू ऐसा है…।
लोकतंत्र में लोक को तिज़ोरी और पेटी में क़ैद करना किसी कला से कम नहीं है।
मैं एक लोक, लोकतंत्र में महज़ तमाशबीन हूँ
एक लद्धड़ खिलाड़ी हूँ
बातें बनाने का खेल भी नहीं आता
मेरे पीछे नाराज़गियाँ छूट जाती हैं
मैं रोशनी की तलाश में भटकता रहा
माचिस भी जलाता हूँ अगर
कभी अँधेरे में तो
मैं केवल अपने अँधेरे में रोशनी ला पाता हूँ
मासूम स्वप्निल आँखें
धँसी हुई नम आँखें दस्तक देती हैं
स्वप्न में
लम्बी धूल भरी राहों में
पतंगों से लदा हुआ बबूल का पेड़ पूछता है
मेरी छाँव में तुम कब आओगे?
आओ!
मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता
घड़े में बंद एक घुटी हुई चीख हूँ
एक और साल
‘कोई साल नहीं’ की तरफ़ जाता है
कोई रास्ता है? तो।
कोई बात नहीं
कोई और साथ नहीं है।
लेकिन मैं यहाँ हूँ।
था।
गा।
जब भी सुकून का कोना खोजता हूँ
रंगों की बन्दूक लिये
नक़ाबपोशों का हमला छीन ले जाता है
चुप रहने का अधिकार कोई छीनता है भला
शांति। कैसी?
खुशी। कैसी?
ऐसे आयोजन जिसमें आमंत्रित नहीं’हूँ।
भटका हुआ परदेशी भर
कौतूहल की पलकों पर बैठा दिया जाता है।
मौन को भरने के लिए बोलता हूँ
मेरी चुप्पी बर्दाश्त के लायक नहीं है
बोलना कहीं ज़्यादा कष्टदायक होता जाता है
वे जानना चाहते हैं। मेरे बारे में। दर्द के नहीं।
हवा ख़राब है। पेट्रोल। शब्द।
फिर भी साँस लेना? है।
घर(तत्व)
समाज(आग)
मैं(ऑक्सीजन)
त्रिविमीय घेरा है
मेरी वजह से झुलसेंगे घर
कठोर से कठोरतर होने पर अमादा
सरल हो जाऊँ तो कहीं का बचूँगा नहीं।
हवा जितना सरल होना चाहत है।
खोटी सरलता
भ्रष्ट भावुकता
नष्ट कर रही है मौलिकता
जटिल होना मौलिक होना है। क्या?
नोट : कभी इसी कविता में लिख दूँगा कि…
कमोड पर बैठे-बैठे
फ्लश हो जाने का ख्याल आता है।
000
डर
जब आसमान काली परछाईं में डूब गया है
धरती अभी-अभी अपनी थरथराहट से उबरी है
जब छोटी-छोटी सर्दियाँ एकदम से बीत जायेंगी
कल की सुबह जब बसंत के आगमन में कालियाँ मुस्कुरायेंगी
मोर, आम के पेड़ों से उड़कर कहीं सरसों के खेतों में होली खेल रहे होंगे
ठीक उससे पहले आज की रात
आज अमावस की काली रात में मेरे कुछ साथी मार दिये गये
इसमें अँधेरे की कोई ग़लती नहीं थी
वे अँधेरे को चीरकर लौटते रहे हैं बार-बार
गोया मेरे कुछ साथी उजाले में मारे गये और किसी को कानों-कान ख़बर नहीं हुई
मरने से ठीक पहले मैंने छुपकर दूर से देखी थी उनकी आँखें
आँखें… मौत के मुँह में जाते हुए
खोजती
अपने घर-परिवार
खेत-खलिहान
सपने और यथार्थ
फिर ऐसा क्या है जो दौड़े चले आये दूर-गाँव हज़ारों-हज़ार
धर्म-ईश्वर-श्रद्धा-भक्ति-पाप-पुण्य-डर
साला! ये आता कहाँ से है डर
एक माँ अपने दुधमुँहे बच्चे से बेपरवाह धर्म में डुबकी लगाती है और फिर नहीं मिलती
एक देशभक्त उघारता है भारतमाता का बदन और निःसंकोच कह देता है कि क्या बुराई है
नदियों में तो ऐसे ही बहती रहती हो तुम
एक मदारी बार-बार लगाता है तमाशा और कराता है मुनादी
सुनो!सुनो!सुनो! चले आओ! चले आओ! चले आओ!
144 साल, जी हाँ! 144 साल बाद आया है संयोग
अभी नहीं तो कभी नहीं
वे जो अपने बच्चों, खलिहानों और दुलरुआ पशुओं से छुपते-छुपाते चली आयीं थीं
और स्वरूप रानी जैसे अस्पतालों के मुर्दाघरों में भी नहीं पायीं गयीं
किस डर ने उन्हें निगल लिया समूचा
ज़िंदा या मुर्दा।
000
pradeepty07@gmail.com





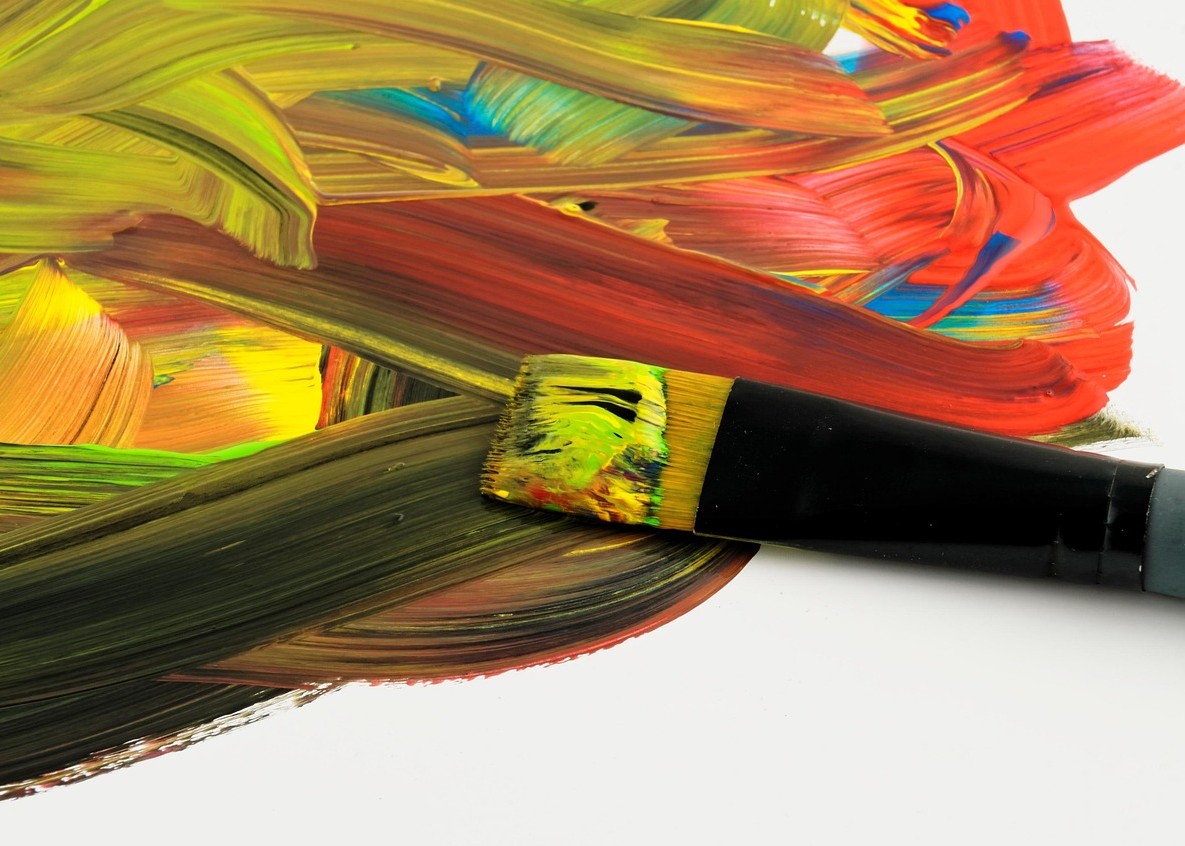



स्मृति से बहुत-कुछ लेकर स्मृति रचती हुई प्रदीप्त की कविताएँ टटकेपन का आभास कराती हैं।
शुक्रिया सर! जलेस जयपुर, कार्यक्रम में आपसे मिलना नहीं हो पाया।
बहुत अच्छी और प्रासंगिक कविताएँ
प्रदीप जी को शुभकामनाएँ
अच्छी कविताएं हैं, नोट कविता का शिल्प और कथ्य बिल्कुल अलग है। बहुत कुछ कहा है पर आक्रोश से नहीं। 🌸
शुक्रिया
आगे बढ़ती कविताएं।
आगे बढ़कर बहुत कुछ कहती कविताएं।
ढेर सारी बधाईयाँ प्रदीप्त …..🌼
मुझे ग्यारह रन और बनाने हैं ..थोड़ा भावुक कर देने वाली है ।
बहुत सुंदर ❤️
बहुत सुंदर कविताए है।