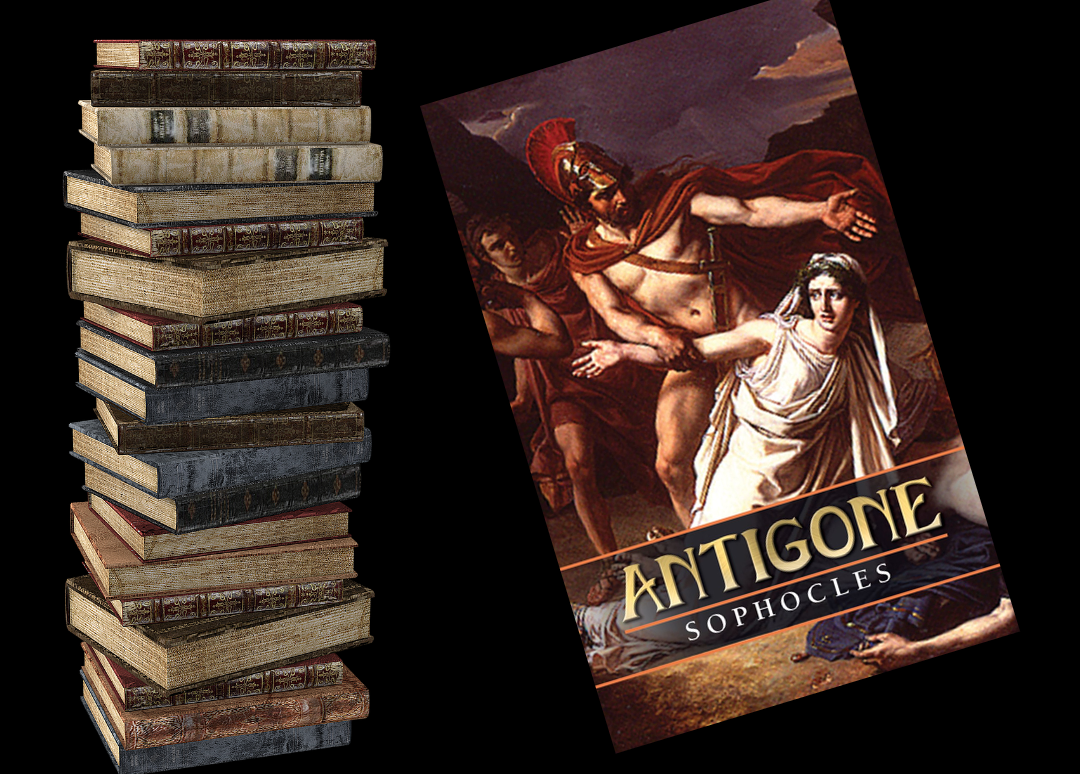‘रूपाली दत्ता और अन्य कविताएँ’ लिखने वाली शानदार कवि ज्योति शोभा का यह यात्रा-संस्मरण जितना दिलचस्प है, उतना ही बहसतलब भी। करने को तो आप इस पर भी बहस कर सकते हैं कि उन्होंने प. बंगाल और केरल में वाम जनवादी मोर्चे के शासन को कम्युनिज़्म कैसे कह दिया जबकि वह पूँजीवादी लोकतंत्र की केंद्रीय व्यवस्था के अधीन था! लेकिन हम भी जानते हैं कि ऐसे मौक़ों पर ‘कम्युनिज़्म’ शब्द का आशय शासन व्यवस्था से नहीं होता। बहस के वाजिब मुद्दे असल में बंगाल और केरल की तुलना में छिपे हैं। स्वागत है!

हमारी गाड़ी कन्नूर की सड़क से गुज़र रही है। दोनों तरफ़ नारियल और केले के दरख़्तों से गुलज़ार हवा। नमकीन सीलन और कम्युनिस्ट पार्टी का निशान हर दिखने वाली चीज़ पर बरक़रार सा दिख रहा है। जो औरत मुझे चाय देती है वह बेहद हँसमुख है और उसकी बगल में रास्ता बताने वाला आदमी सुलझा हुआ, भाषा में एकदम खुला।
केरल में कम्युनिज़्म, यह विचारधारा सिर्फ़ दीवारों, झण्डों और पोस्टर पर नहीं बल्कि दरिया की लहरों पर भी लिखी हुई है, जैसे लोगों के चेहरों पर भी। बेहद गर्व से भरे विनम्र चेहरे। एक जीवन दृष्टि जो अब सौ साल की हो चली और नंबूदिरीपाद के बाद पिनाराई विजयन के रूप में उतनी ही लोकप्रिय है।
मुझे हैरत है, यहाँ केरल में इसकी गति और प्रगति देख कर। मैं इसे बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देख रही हूँ। दो राज्यों की शक्ल एक विचारधारा के भीतर इतनी अलग कैसे है? दो राज्य जिनके मिज़ाज एक जैसे हो सकते थे, वे विपरीत क्यों ? शायद इस सवाल का जवाब इतिहास में है, उस समय के पहिये में है जो आज़ादी के बाद से लगातार एक धुरी पर न घूम कर अपनी जगह बदलता रहा, दिशा बदलता रहा और चेहरे बदलता रहा।
1957 में कम्युनिज़्म का जन्म केरल में होने का पहला कारण यह रहा होगा कि विश्व सभ्यता से पहला परिचय भारत का यहीं से हुआ। पुर्तगाली और अंग्रेजी शासन की पहली सीढ़ी यही थी। एक सर्वाधिक पिछड़ा प्रदेश जहाँ सामंती प्रथा चरम पर थी और समाज के दो तबकों के बीच गहरी खाई थी। निचले तबके का जीवन नर्क जैसा था। जिसे 1892 में अपनी दक्षिणी यात्रा के दौरान विवेकानंद ने भी लक्षित किया था। हद से बाहर शोषण और समाज की संरचना बेहद अमानवीय। यानी एक ठोस ज़मीन तैयार हुई थी इस विचारधारा के लिए, जिसका वादा था कि पूंजीवाद और सामंती प्रथा से मुक्ति मिलेगी, बराबरी का अधिकार होगा और एक सुंदर सामाजिक व्यवस्था क़ायम होगी। कोई हैरत नहीं कि दक्षिण का यह हिस्सा उन दिनों बेहद परम्परावादी होने के साथ पितृसत्तावादी था। औरतों और दलितों की स्थिति बदतर थी। अछूत इतने अछूत थे कि उनकी छाया भी हवा को दूषित कर देती थी। शायद यही हालात थे जो केरल में असंतोष और विस्फोट की वजह बने और यहाँ लगभग हर समुदाय ने कम्युनिज़्म का स्वागत हाथों हाथ किया। तब वह पार्टी उभरी जिसकी स्थापना एक विचारधारा से शुरू हुई थी और आने वाले वर्षों में वह प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सामने रही। उसने चीन के उदाहरण को सामने रखा और यह विश्वास दिलाया कि एक रहने योग्य समाज का सपना इतना बड़ा न था कि लोग उसे कभी न देखें। हालाँकि बाद के वर्षों में यह सपना कितना साकार हुआ और कितना बिखरा, यह पहचानी सी दास्तान है। इसकी ज़द में कितने ही राज्य (बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा) आये और विचारधारा के धीमे पड़ते बहाव से छूट गए।
मगर आज जब मैं वायनाड और कन्नूर के लोगों से मिलती हूँ तो उनकी निश्छल हँसी से लगता है कि वह स्वप्न शायद थोड़ा ही सही, साकार तो हुआ होगा। वह स्वप्न जो केरल की हरीतिमा में घुला मिला दिख रहा है, उसमें कोई तो बात रही होगी जो इन ऊँची नीची पहाड़ियों पर बने सुंदर घर और इनके सुरुचिपूर्ण रख रखाव में दीखता है। चारों ओर जंगल हैं, पानी है, मगर उनके घर के फर्श पर एक धब्बा नहीं। रसोई खुशबूदार है और दिल खुले। मेरे होम स्टे के कर्ताधर्ता मुरली सर की बूढ़ी आँखों में अजब सी चमक है। साफ़ अंग्रेजी में और थोड़ी टूटी हिंदी में वे कहते हैं कि वे फॉरेस्ट अफसर थे और उनकी बीवी रबर प्लान्टेशन देखती थी। हमने यह प्रॉपर्टी उसी रबर प्लान्टेशन को बेच कर ख़रीदी है और बच्चे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे यक़ीन है , यह इतनी सहज बात नहीं, मगर यह इतनी विनम्रता से कही जाती है कि एक पल को जैसे मन छू कर निकल जाती है। मैं सोचती हूँ, यह अनायास तो नहीं कि फूलों के पौधों के बीच जहाँ कोई बेतुका इश्तेहार मुँह चिढ़ा सकता था, वहाँ लाल कपड़े पर बना हँसिया और हथौड़ा लहरा रहा है। ज़िंदादिली ऐसी है उस उम्रदराज़ अफसर की, कि चाय ख़त्म होने के बाद भी वे करीब ही बैठे रहते हैं। मैं कहती हूँ – आपका यह घर मुझे पसंद है तो वे बच्चों की तरह पुलक से भर उठते हैं। दुनिया जहाँ में उनकी दिलचस्पी अपने घर से शुरू हो रही है। उनकी मुस्कराहट इन्फेक्शस है जो मुझे भी मुस्कुराने पर मजबूर करती है।

इंसानी ज़िन्दगी और एक नागरिक के तौर पर हासिल इस परिणाम को मैं बंगाल के समकक्ष रखती हूँ तो महसूस होता है कि वह जंग जो मूलभूत मुद्दों पर टिकी होती है, उसकी परिणीति केरल की तरह होती होगी। नंबूदिरीपाद एक नेता से अधिक लोगों के बीच एक साधारण नागरिक की तरह सामने आए जिसे इस बदहाली में बदलाव की दरकार थी। बदलाव हुए, तरक्की हुई। कम्युनिज़्म की सफलता में हाथ रहा इनके दूरदर्शी नेताओं की सोच का और सबसे अधिक जनता की जागरूकता का जो आज अपनी साक्षरता और ख़ुशहाली पर गर्व कर सकती है। यह और बात है कि केरल में इस प्रक्रिया को एक लम्बे संघर्ष से गुज़रना पड़ा, यह भी विस्थापन के दर्द से अछूता न रहा। इसने भी वे तमाम दर्द झेले हैं जिसने लगभग देश के सभी सीमावर्ती राज्यों को अरसे तक अराजकता में रखा है। मगर एक सबसे अच्छी बात जो बाद के वर्षों में हुई वह यह रही कि दो बड़ी पार्टियों, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच तना तनी बनी रही यहाँ और सत्ता पर कब्ज़ा बनाये रखने के संघर्ष ने उन्हें अराजक न होने दिया जो बंगाल की सबसे बड़ी कमी रही।
बंगाल में पार्टी अपने को दिशाहीन होने से नहीं रोक पाई। 1971 में बंगाल में सत्ता में आने के बाद इस विचारधारा से उम्मीद बेतहाशा थी। विभाजन के बाद हुए पलायन से बंगाल टूटा बिखरा था, लोग बेरोज़गार । ट्रेड यूनियन और कारोबारियों के लम्बे झगड़े में मज़दूर तबाह हो चुके थे। मगर कम्युनिस्ट के शुरूआती नेता ज्योति बसु की नीतियों में संभवतः बंगाल विभाजन के नुकसान की भरपाई करने की क्षमता से अधिक सत्ता पर काबिज़ रहने की नीति थी । यहाँ की जनता में वह सजगता भी नहीं रही कि वह आगे जाने की राह बनाए और सत्ताधारी सुनिश्चित करें कि पंचायत स्तर पर काम हो जिसे केरल में कम्युनिज़्म की सफलता के बाद केरल मॉडल कहा गया था। वह मॉडल जो जीडीपी के लिहाज़ से ज़्यादा क़ामयाब न हो कर भी मानव विकास सूचनांक में आगे है। इसे महज़ संयोग तो नहीं कहेंगे कि कम्युनिज़्म यहाँ तीन से अधिक दशकों के निर्विरोध शासन के बाद भी असफल हो गया। जो व्यवस्था पूंजीवाद के हाथों में पहले थी वह जस की तस बनी रही। भद्रलोक अपने संसाधनों के संग सुरक्षित रहे, वंचित सामाजिक हाशिए में और पीछे धकेल दिए गए। बंगाल में इसने नागरिकों को वह गर्व नहीं दिया जो शिक्षा और रोजगार के संग आता है।
अभी वायनाड के एक रेस्त्रां में मेरे सामने एक दरभंगा का एक लड़का थाली में ख़त्म हो चुकी सब्ज़ी डाल रहा है और धड़ल्ले से मलयाली में बात करता है। मैं पूछती हूँ – क्या अच्छा लगता है यहाँ? वह मुस्कुराता है। उनकी आँखें चमकती हैं। मेरे दिल में एक हूक सी उठती है। 34 बरसों की कम्युनिस्ट सत्ता में बंगाल में मैंने यह जुनून नहीं देखा जो यहाँ केरल के सामान्य आदमी के चेहरे पर देखा आज। विजयन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मगर मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है वेणुगोपाल मंदिर के बाहर चाय के संग बचे हुए मुरक्कू नारियल की सुतली से बाँध कर देती ललिता और होम स्टे की सुधा अम्मा, जो मेरी रात की थाली में केरल की सबसे मीठी पायसम ले कर आती हैं। लौटती बेला जब तेज़ी से भागते दृश्य में नारियल के पेड़ और चाय बागानों की हरीतिमा पीछे छूटती है तो मन यहीं रह जाना चाहता है। मैं उलझन में पड़ जाती हूँ कि इसे मैं किसकी जीत मानूँ – कम्युनिज़्म की या इन ज़िंदादिल लोगों की?
jyotimodi1977@gmail.com