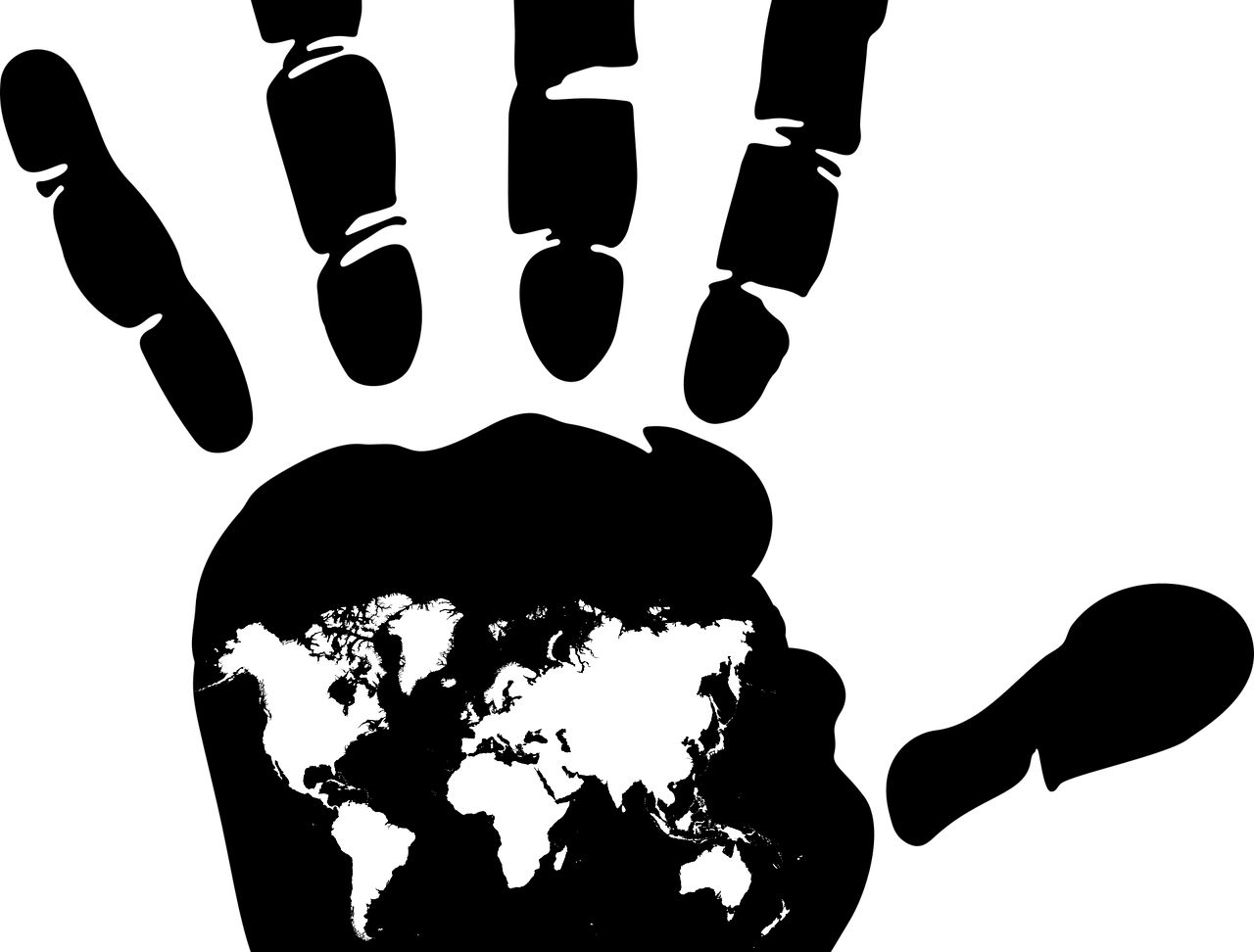इरफ़ान हबीब का यह निबंध –दि नेशन दैट इज़ इंडिया–पहले पहल 10 जून 2003 को ‘दी लिटिल मैगज़ीन’ में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद इसका विस्तृत रूप ‘काउंटरकरेंट्स’ (Countercurrents.org) द्वारा प्रकाशित किया गया (https://www.countercurrents.org/comm-habib100603.htm )। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है भावुक और विष्णु प्रभाकर उपाध्याय ने। भावुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के शोधछात्र हैं और विष्णु प्रभाकर उपाध्याय वहीं हिंदी विभाग में शोधछात्र हैं।

1983 में जब बेनेडिक्ट ऐंडरसन की किताब इमैजिन्ड कम्यूनिटीज़: रिफ्लेक्शंस ऑन दी ओरिजिन्स एंड स्प्रैड ऑफ़ नैशनलिज़्म (‘काल्पनिक समुदाय: राष्ट्रवाद के आरंभ और प्रस्फुटन पर एक विमर्श’) प्रकाशित हुई, तब इसे पश्चिमी यूरोप से बाहर के लोगों ने राष्ट्रीयता के दावे की एक निरुत्तर कर देनेवाली आलोचना के तौर पर देखा। ऐंडरसन के पाठकों में ऐसे लोग बहुत ही कम थे जिन्होंने इस बात पर ग़ौर किया कि इमैजिन्ड (काल्पनिक) शब्द के ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब निकाले जा रहे थे। ऐंडरसन से पहले अन्य लेखक भी चेतना, आस्था, मान्यता आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा इस ओर इशारा कर चुके थे कि एक राष्ट्र तब अस्तित्व में आता है जब उसके एक विशाल समूह को यह निश्चित हो जाता है कि वे सब मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। मगर एक लिहाज़ से राष्ट्र किसी संस्था या समुदाय जैसा ही है, चाहें हम धार्मिक समुदाय की बात करें, या परिवार की, या जनजाति की, और यहाँ तक कि किसी पेशे की भी। यह हमारी अवधारणा ही है जो हमें एक पंथ, एक वंश अथवा एक ही तरीक़े से काम करने में सहभागी होने के एहसास के ज़रिये एक ही वर्ग या संप्रदाय से होने की दृष्टि देती है। अतः यह हमारी कल्पना या अवधारणा ही है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है।
यदि ऐंडरसन की किताब में कोई ऐसी बात है जिसे दोहराना फ़ायदेमंद होगा तो वह यह है कि राष्ट्रीयता की अवधारणा एक नये दौर, एक नयी प्रवृत्ति की है। पश्चिमी यूरोप से बाहर ज़्यादातर विश्व में यह मुख्यतः फ्रांसीसी क्रांति (1789) के बाद की घटना है। ऐंडरसन हमें बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के रोमांचकारी विचारों ने बोलीवर से आरंभ होते हुए लैटिन अमेरिका के महत्वाकांक्षी युवकों को अपनी गिरफ़्त में लिया, लेकिन हक़ीक़त में ऐसा नहीं था। राष्ट्रवाद के फ़रोग़ (विकास) के लिए एक महत्वपूर्ण आधार उपनिवेशवाद ने प्रदान किया जो न लैटिन अमेरिका, न एशिया और न अफ़्रीका के लिए किसी भी तरह से काल्पनिक घटना थी। उपनिवेशवाद निर्दयी तौर पर शोषणकारी था और उसकी मुख़ालफ़त तभी मुमकिन थी जब शोषित जनता को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाता। “राष्ट्र” ठीक ऐसी ही एकजुटता के लिए एक मंच प्रदान कर रहा था।
अनजाने में ही सही मगर उपनिवेशवाद विचारों के संप्रेषण का बहुत शानदार माध्यम भी था। अपना आधार यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किये हुए इस उपनिवेशवाद का आर्थिक ढाँचा महानगरीय (मेट्रोपॉलिटन) देशों की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पर निर्भर था। यह उपनिवेशवाद के अपने हक़ में था कि पूँजीवाद के कुछ तत्व जैसे रेलवे, उत्पादन के लिए फैक्ट्रियाँ और कुछ तकनीकें उपनिवेशों तक पहुँचें और उपनिवेशी आबादी का कुछ हिस्सा वहाँ का निज़ाम चलाने की सहूलियत की ग़र्ज़ से शासकों की भाषा सीखे। इन सबने यूरोप से विचारों और ज्ञान के आगमन के रास्ते खोल दिये। मार्क्स ने इसे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अदा किये विघटनकारी किरदार के बरअक्स शोषित लोगों की तरक्क़ी का ज़रिया बताया है। मार्क्स ने 1853 में यह बात भारत ही के संदर्भ में की थी। विघटनकारी और उत्थानकारी प्रक्रियाओं की इस धारणा को ऐडवर्ड सईद ने अपनी किताब ओरिएंटलिज़्म में चुनौती दी। इसका पहला संस्करण 1978 में आया था। 1995 के नये संस्करण में जोड़े गये निष्कर्ष में अपने इनकारिया बयान के बावजूद सईद स्पष्ट तौर पर यह दलील देते हैं कि यूरोप द्वारा पूर्वी देशों और उनके लोगों के अध्ययन ने उनकी संस्कृति का एक विकृत रूप दुनिया के सामने पेश किया है। इसके बाद जल्द ही लोग उपनिवेशी संवाद (बात-चीत), यहाँ तक कि उपनिवेशी ज्ञान के बारे में भी सुनने लगे। 1990 में प्रकाशित हुई रोलैंड इंडेन की पुस्तक इमैजिनिंग इंडिया में रोलैंड ने पहले पहल कहा कि इन प्राच्यवादी शिक्षाओं के अंतर्गत भारतीयों की अपनी समझ, अपनी दुनिया बनाने की उनकी क्षमता को विस्थापित कर किसी दूसरी शक्ति को दे दिया गया। यहाँ शिक्षा के स्थान पर बहुवचन “शिक्षाओं” का इस्तेमाल दिखाता है कि अब हम उत्तर-आधुनिकतावाद की जानकारियों के ढाँचों की ओर बढ़ चले हैं।
अपनी पुस्तक की परिशिष्ट में सईद कहते हैं कि मैं प्राच्यवादियों की तकनीकी उपलब्धियों को नहीं नकारना चाह रहा हूँ किंतु उन्हें कुछ ठहरकर इस बात पर विचार करना चाहिए था कि इन तकनीकी तत्वों से असल में हुआ क्या? ये तकनीकी तत्व इस दृष्टिकोण को मज़बूत करते हैं कि गैर-यूरोपीय लोगों को भी उन्हीं तरीक़ों और कसौटियों द्वारा परखा जा सकता है जिनके द्वारा यूरोपीय लोगों को। कुछ लोगों की यह अवधारणा कि वह दूसरों से अलग हैं और अपने में श्रेष्ठ हैं, जो कि उपनिवेशवाद के आख्यान का शुरुआती बिंदु हुआ करती थी, वह प्राच्यवादियों के लगातार वैज्ञानिक पद्धति को समान रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत से चुनौती पाती थी। इसी कारण प्राच्यवादियों की एक पीढ़ी द्वारा की गयी भूल या बनाये गये पूर्वाग्रहों को उन्हीं की अगली पीढ़ी उजागर भी करती थी और नकार भी देती थी।
बहुत से ऐसे देश बने हैं जिनका पहले से एक देश के रूप में अस्तित्व नहीं था जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इक्वाडोर, बोलिविया, कॉन्गो इत्यादि, लेकिन ये सभी ऐसी जगहों पर हैं जहाँ किसी न किसी वजह से राष्ट्र का तसव्वुर ही नामौजूद था। जहाँ ऐसा तसव्वुर आधुनिक दौर से पहले मौजूद था, वहाँ लोगों के दिमाग़ में स्थापित देश स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीयता का पात्र बन जाता है। साफ़ तौर पर यही कारण है कि बाथवादियों अथवा नास्सरीय मिस्र को मिस्र, सीरिया और ईराक़ के अलग देशों के स्थान पर एक संयुक्त और अटूट “अरब राष्ट्र” बनाने में बेइंतहा मुश्किलें पेश आती रही हैं। यदि ग़ौर किया जाए तो यह तो सार्वभौमिकता की अवधारणा है जिसने पश्चिम से पूर्व की ओर विचारों का आदान-प्रदान मुमकिन बनाया है। आज़ादी, संविधान और राष्ट्र केवल यूरोप के लिए ही मुफ़ीद सिद्धांत नहीं थे बल्कि सामान परिस्थितियों में पूरे मानव समाज पर समान रूप से लागू होते थे। इसी कारण यह विश्वास पैदा हुआ कि पूर्व (ईस्ट) में मौजूद देश भी राष्ट्र हो सकते हैं।
जब 1830 के एक पत्र में राजा राममोहन रॉय ने लिखा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है क्योंकि भारतीय जातियों में बँटे हुए हैं, तब उन्होंने गूढ़ रूप से यह भी क़बूल किया कि यदि भारतीय जाति से हटकर देश को प्राथमिकता दें तो वह एक राष्ट्र बन सकते हैं। केशव चंद्र सेन भारत में शिक्षा के विकास और सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रकाश में 1870 में ही इस संभावना पर विचार कर रहे थे। नरम दलीय नेताओं द्वारा 1885 में मुंबई में स्थापित की गयी संस्था को दिये नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, से ही इस तथ्य को बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता प्रदान कर दी गयी कि भारत एक राष्ट्र है। लेकिन सवाल यह बनता है कि भारत को ही क्यों राष्ट्र के तौर पर चुना गया, उसमें मौजूद भूमिगत इकाइयों को क्यों नहीं? ऐसा शायद इसलिए कि केवल भारत को ही एक राष्ट्र के तौर पर देखा जाता था। एक राष्ट्र के तौर पर भारत का अस्तित्व अंग्रेज़ी हुकूमत से बहुत पहले से था। बिला शुबा इसके कारणों में भौगोलिक यथार्थ के तत्वों का भी योगदान था, जैसे भारतीय प्रायद्वीप को यूरोपीय महाद्वीप से अलग करते हुए पहाड़ और दरिया। इन सीमाओं के भीतर साझा संस्कृति और सांस्कृतिक अपनत्व पैदा हो चुका था जिसके आधार पर लोग भारतीयों को विश्व के बाक़ी लोगों से अलग रूप में देखा करते थे।
अपनत्व की इन बातों में से कई ऐसी हैं जो हिंदू रिवायत की मानी जा सकती हैं। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वैचारिकी और कर्मकांड साझा सांस्कृतिक तत्वों के महत्वपूर्ण अंग थे। लेकिन इस बात को अवश्य दर्शाया जा सकता है कि राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा संस्कृत में लिखने वाले किसी भी लेखक से ज़्यादा सशक्त फ़ारसी में लिखने वाले लेखकों मसलन अमीर खुसरो और अबुल फ़ज़ल में है, जैसा कि मैंने अपने दो निबंधों में दिखाने का प्रयास किया है। ऐसा इसलिए है कि सांस्कृतिक समानताएँ खालिसतन धार्मिक नहीं थीं। ताराचंद अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ़ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर में यह बताते हैं कि विस्तृत राजनीतिक ढाँचों, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने विस्तृत राजनीतिक निष्ठाओं को बढ़ावा देने का काम किया और इसने राष्ट्र की एकता की अवधारणा को और मज़बूत किया। यहाँ तक कि 18वीं सदी में जब वह अपनी सारी ताक़त खो चुका था, तब भी मुग़ल बादशाह को ही हिंदुस्तान का स्वाभाविक शासक तसव्वुर किया जाता था। यहाँ तक कि जब अवध के विद्रोहियों ने बिरजिस क़ादिर के नाम पर महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा के विरोध में अपना जवाब लिखा, तब उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा हिंदुस्तान के राजाओं पर किये गये अत्याचार की बात की जिसमें उन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान और पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह, दोनों का ही ज़िक्र किया। उनके शब्दों में, यह हिंदुस्तान के लोग और यहाँ की सेवा है जो अब अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए उठ खड़ी हुई है। अतः 1857 के विद्रोहियों ने भारत को स्पष्ट तौर पर अपने राष्ट्र के रूप में देखा और यहाँ के लोगों को अपने स्वाभाविक सहयोगियों के रूप में। इसके बावजूद यदि उनकी कल्पना का भारत एक राष्ट्र नहीं था तो वह सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें पूरे देश में एक राज्य स्थापित करने का ख्याल नहीं आया था और एक एकीकृत (संयुक्त) राजनीतिक सत्ता ही राष्ट्रवाद का मूल है।
आर्थिक तौर पर राष्ट्र का एकीकरण 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में रेलवे निर्माण और टेलीग्राफ सुविधा शुरू होने के कारण आरंभ हुआ था। यह सभी ऐसे क़दम थे जो औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपने फ़ायदे के लिए उठाये गये थे किंतु नये संचार माध्यमों के कारण प्रशासन के केंद्रीकरण ने भारतीयों को भारत को एक संभावित एकीकृत राजनीतिक इकाई के तौर पर देखने में सहायता की। मुख्य तौर पर भारतीयों के अपने प्रयासों की देन, आधुनिक शिक्षा और प्रेस के विकास ने भारतीय राष्ट्रीयता और संवैधानिक सुधारों के विचार को प्रसारित किया। भारतीय राष्ट्रीयता के लिए एक ठोस आधार की नींव तब रखी गयी जब दादाभाई नरौजी (पॉवर्टी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901) और आर.सी. दत्त (इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, दो जिल्द में 1901 और 1903) जैसे राष्ट्रवादियों ने भारतीयों की ग़रीबी और इसके लिए ज़िम्मेदार औपनिवेशिक शोषण का मुद्दा उठाया जिसका असर पूरे भारत में समान रूप से महसूस किया जा रहा था।
अतः हम देखते हैं कि तीन पेचीदा प्रक्रियाएँ समानांतर तौर पर काम करती हैं जिसके कारण भारत का एक राष्ट्र के तौर पर उदय होता है। यह तीन प्रक्रियाएँ हैं: भारत का राष्ट्र के तौर पर माज़ी में तसव्वुर, आधुनिक राजनीतिक विचारों का आगमन, और उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष। इनमें से अंतिम प्रक्रिया निर्णायक थी और इसीलिए भारतीय राष्ट्र के निर्माण को राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है।
यह विचार जो माज़ी में पेश किया गया था, उसे कई निंदकों से बचाना भी ज़रूरी था। साइमन कमीशन रिपोर्ट (1930) ने इस ओर इशारा किया कि भारत में सांस्कृतिक विविधताएँ, धार्मिक विभेद और बहुतायत भाषाएँ हैं। इस तथ्य पर स्विट्जरलैंड का क्लासिक उदाहरण देकर प्रतिघात तो किया जा सकता था जहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों मत के लोग हैं और चार भाषाएँ बोली जाती हैं, मगर इस तकनीकी गुत्थम-गुत्थी से आगे जाकर लोगों को एक स्वतंत्र और एकीकृत भारत में होने वाले लाभों से अवगत कराया जाना ज़्यादा ज़रूरी था। यही कारण है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट का असल जवाब मार्च 1931 में पारित हुआ कराची प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने भविष्य के आज़ाद भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आयाम पेश किये जिनके तहत राज्य सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। इस प्रस्ताव द्वारा यह प्रतिज्ञा की गयी कि भारतीय राज्य सभी धर्म को लेकर निष्पक्षता का मुज़ाहिरा करेगा और विभिन्न भाषाई इलाकों की संस्कृति और भाषा की रक्षा करेगा।
धार्मिक विभेदों ने निश्चित तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष एवं एकीकृत भारतीय राष्ट्र के तसव्वुर को कमज़ोर किया। यह तो जग-ज़ाहिर समझ कर मान ही लिया जाना चाहिए कि “फूट डालो और राज करो” की नीति उपनिवेशवाद के लिए बेहद लाभकारी थी। हालाँकि ऐसी नीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती थी जब तक कि देश में विभाजन के कुछ बीज मौजूद नहीं होते। वही सब नयी परिस्थितियाँ जिन्होंने राष्ट्रीय उद्देश्य का बहुत हित किया था, उन्हीं ने हिंदू और मुस्लिम दोनों साम्प्रदायिकताओं को इतने बड़े पैमाने पर एक मंच प्रदान किया जिसकी 1857 से पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसमें सबसे अहम किरदार था संचार के तेज़ माध्यम और प्रेस का। अपने शुरुआती दौर में एक प्रकार के राष्ट्रवाद ने धर्म का सहारा भी लिया क्योंकि वह जन समूह को इकट्ठा करने के अन्य घटकों की अनुपस्थिति में मोबिलाइज़ेशन का बहुत कारगार स्रोत था। 1890 में age of consent बिल (सहमति की आयु अधिनियम) और महामारी (प्लेग) से बचाव के लिए टीकाकरण के ख़िलाफ़ तिलक के विरोध-प्रदर्शन के साथ-साथ उनका शिवाजी के व्यक्तित्व के गिर्द भक्ति को प्रेरित करना इस प्रवृत्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण है। साथ ही साथ अरविंद घोष हिंदू राष्ट्रवाद के लिए एक सैद्धांतिक आधार तैयार कर चुके थे। ठीक इसी प्रकार तिलक के एक वरिष्ठ समकालीन जमालुद्दीन अफ़ग़ानी ने पैनइस्लामिज़्म के सिद्धांत को प्रसारित करते हुए सभी मुसलमानों को यूरोपीय औपनिवेशिक ताक़तों के ख़िलाफ़ एक होने के लिए प्रेरित किया और यहाँ भी संगठित करने वाली ताक़त धर्म की ही थी। अफ़ग़ानी के भारत को इस योजना में शामिल न रखने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं था कि किसी वक़्त प्रसारित किये गये इस पैनइस्लामिक तसव्वुर का असर भारतीय मुसलमानों के ज़ेहन पर नहीं पड़ेगा।
राष्ट्रीय एकजुटता के माध्यम जब राजनीतिक और आर्थिक आयाम की ओर मुख़ातिब हुए, तब स्वाभाविक था कि सांप्रदायिक राजनीति में मौजूद उपनिवेशवाद-विरोधी तत्त्व कमज़ोर पड़ने लगे। लंबे समय तक (1893-1914) दक्षिण अफ़्रीका में रहे गांधीजी ने अपने आवास के दौरान भारतीयों को उनके नागरिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध हेतु एकजुट किया था। अतः वे अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि राष्ट्र का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को एकतापूर्वक रहना चाहिए। उनका मानना था कि इंडियन काउन्सिल्स एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों को मिलने वाली रियायतों का विरोध करना हिन्दू नेताओं की तरफ़ से एक ग़लत क़दम था। अपनी दृढ़ धार्मिक मान्यताओं के बावजूद गांधी इसी मत पर अड़े रहे और इसी की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवायी। किंतु यदि भारत में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय मानने वाले नेताओं में गांधी शिखर पर विराजमान थे, तो यह कहना भी ज़रूरी हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने, वाम और क्रांतिकारियों ने भी गांधी के इस विचार में साथ दिया और एक आज़ाद और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की उत्पत्ति सुनिश्चित की।
जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता गया, सांप्रदायिकता की देशभक्ति की साख कमजोर पड़ती गयी। निःसंदेह इसी से ‘द्वि-राष्ट्र’ का सिद्धांत पैदा हुआ, जिसमें ‘अन्य’ राष्ट्र को मुख्य दुश्मन और अंग्रेजों को अपने संभावित सहयोगी के रूप में देखा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने, जिसकी स्थापना 1925 में हुई, हिंदू महासभा से “हिंदू-हिंदी-हिंदुस्तान” का नारा लिया; और 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कांफ्रेंस में दिये डॉ. सर मोहम्मद इक़बाल के भाषण से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की धारणा ने जड़ पकड़ ली, जब तक कि मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव (1940) ने स्पष्ट रूप से अलग राष्ट्र पाकिस्तान (बिना नाम के) के लक्ष्य को पारित नहीं किया। अपनी आत्मकथा में, जवाहरलाल नेहरू ने यह अंतर्दृष्टिपूर्ण टिप्पणी की कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता खुद को राष्ट्रवाद के मुखौटे में छुपा सकती है जबकि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को आसानी से पहचाना जा सकता है कि वह क्या है। आज की सांप्रदायिकता के अनेक मुखौटों की तरह राष्ट्रवादी ‘आवरण’ भी जल्दी ही हट गया, मुस्लिम लीग की तरह, न तो हिंदू महासभा और न ही आरएसएस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-31) के बाद के किसी भी प्रमुख राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लिया।
1947 में स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन निःसंदेह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक झटका था। यद्यपि इस उपलब्धि के लिए उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व को श्रेय दिया जाना चाहिए कि भारत ने अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाये रखा और 1949 के भारतीय संविधान में कराची प्रस्ताव के सिद्धांतों को शामिल किया। क़ानून में बहुत से समझौते और भूलें हुई हैं, व्यवहार में तो और भी ज़्यादा, लेकिन इससे इन उपलब्धियों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता।
अब जब तक़सीम को हुए आधी सदी गुज़र चुकी है, इसको स्वीकार न करना मूर्खता ही होगी कि भारतीय राष्ट्र की सीमाएँ फिर से परिभाषित की गयी हैं, चाहे वो अच्छी हो या न हो। दो राष्ट्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वास्तविकताएँ हैं; और ‘अखंड भारत’ (अविभाजित भारत) का रोना रोना एक गैर-ज़िम्मेदाराना हरक़त से ज्यादा और नहीं हो सकता, जिसकी माँग उन्होंने ही फिर से उठायी है जिनके छिपे हुए दो-राष्ट्र के सिद्धांत ने विभाजन में बड़ा योगदान दिया था। कोई भी इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि हमारे उपमहाद्वीप की एक साझा सांस्कृतिक विरासत है; और आशा है कि एक समय ऐसा भी आयेगा जब इसे बिना किसी शर्मिंदगी के हर तरफ़ से मान्यता दी जायेगी। लेकिन आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि भारत का एक राष्ट्र के रूप में भविष्य क्या है।
इस सवाल को कुछ दुख के साथ पूछा जा सकता है। सोवियत संघ और यूगोस्लाविया जैसे मज़बूत राष्ट्र नक्शे से ग़ायब हो गये हैं। तथ्यात्मकता की तरफ़ लगभग झुक कर एक शुष्कता के साथ ब्रिटिश इतिहासकार इस पर चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन बिना इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में विघटित हुए और कितने समय तक एक राष्ट्र के रूप में बना रह सकता है। भारत जो कि एक बहुत बड़ा देश है, इसमें अलग-अलग क्षेत्र हैं जिन्हें कराची प्रस्ताव में ‘भाषाई क्षेत्र’ कहा गया है। सैद्धांतिक मूल्यों में अत्याधिक विश्वास रखने वाले लोग लंबे समय से इन्हें संभावित राष्ट्रीयताओं के रूप में देखते आए हैं।
1920-21 ई में कांग्रेस ने जब भाषाई क्षेत्रों के आधार पर अपनी प्रांतीय समितियों का गठन किया, तो कांग्रेस ने प्रत्येक क्षेत्र में वहाँ की भाषा को बोलने वालों पर मातृभाषा के शक्तिशाली प्रभाव को ध्यान में रखा। असल में 1956 में, राज्यों के पुनर्गठन ने भारतीय संघ को भाषाई क्षेत्रों के संघ के रूप में फिर से परिभाषित किया। कुल मिलाकर यह प्रयोग सफल रहा।
निःसंदेह आज़ादी के चार दशकों में भारत ने बुनियादी उद्योगों के निर्माण के साथ विकास को देखा जिसने यक़ीन बनाये रखा कि एकता से ही सभी क्षेत्रों को फ़ायदा पहुँचेगा। हालाँकि 1990 के दशक से जब भारत ने ‘निजीकरण’ और ‘वैश्वीकरण’ की प्रक्रियाओं को अपनाया, तब से भारतीय राज्य आर्थिक विकास के लिए और कम प्रासंगिक होता जा रहा है। इसी कारण अब स्थिति बदल गयी है या बहुत तेज़ी से बदल रही है। क्या इस तरह की परिस्थितियों में बेहतर स्थिति वाले राज्यों की आकांक्षाओं या कम संसाधनयुक्त लोगों की चिंताओं को एक साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जा सकता है?
सांस्कृतिक मतभेदों की भी बात है। भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था पर अपनी विचारधारा को थोपने पर आमादा है कि भारतीय संस्कृति का एकमात्र स्रोत वेद हैं, द्रविड़ भाषाएं वैदिक संस्कृत से निकली हैं और सिंधु सभ्यता आर्यन सभ्यता है न कि द्रविड़। इसके अलावा स्कूली पाठ्यक्रमों में मुस्लिम और ईसाई विरोधी पूर्वाग्रहों को शामिल किया जा रहा है जिसका चरित्र स्पष्टतः विभाजनकारी है। कोई नहीं जानता है कि आने वाले समय में हमारी राष्ट्रीय एकता पर इसका क्या असर होगा। मिसाल के तौर पर, एक कश्मीरी या एक तमिल छात्र की इस तरह की संकीर्णता पर क्या प्रतिक्रिया होगी?
मेरा मानना है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन यह आर्थिक रूप से सक्रिय, महत्वाकांक्षी कल्याणकारी राज्य से निकटता से जुड़ा हुआ है और साथ ही यह वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष मानसिकता से भी उतनी ही निकटता से जुड़ा हुआ है। सांप्रदायिकता और संकीर्णता इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, चाहे वे ऊपर से कितना भी राष्ट्रवादी मुखौटा पहनें। आशा है कि भारतीय लोग भारतीय राष्ट्र के दृष्टिकोण को बनाये रखेंगे और इसे कमज़ोर करने वाली हर चीज़ को ख़ारिज कर देंगे।
अनुवादक-द्वय :
bhavuksharma30@gmail.com / vishnu.prabhakar708@gmail.com