“ये लघुकथाएं एक संक्षिप्त काल की हैं, फिर भी लेखक ने परिस्थितियों, विचारों और बयान करने की कला को दोहराने से बचने की सावधानी बरती है।”–मलीहुज़्ज़मां (एम ज़ेड ख़ां) के संग्रह पर अली इमाम ख़ां का समीक्षा-लेख।

झारखण्ड के मलीहुज़्ज़मां (जो एम.ज़ेड. ख़ां के नाम से जाने जाते हैं) के उर्दू अफ़सांचों (लघुकथाओं) के संग्रह क्वारंटाइन सेन्टर में मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक लिखी गई 61 लघुकथाएं हैं। ये लघुकथाएं कोरोना महामारी की विभीषिका, मौत के मंडराते साये, वातावरण में व्याप्त भय एवं दहशत, अपनों के असमय खोने का दर्द और ग़म, रिश्तों का संकट, हर तरफ़ अफ़रा-तफ़री का माहौल, उजड़ते आशियाने, बंद होते रोज़गार और बेकार होते लोग, प्रवासी मज़दूरों का विस्थापन और घरों की ओर बिना तैयारी, बिना ज़रूरी साज व सामान के विपरीत पलायन की पीड़ा झेलते, किसी तरह जान बचाने की चिंता में जान गंवाते एवं अपने घरों से दूर बीच में फंसे न जीते न मरते लोग, लाॅकडाउन में यातायात के साधनों का अभाव, श्रमिक ट्रेनों का बुरा हाल , क्वारंटाइन सेन्टर की कुव्यवस्था , दवाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की घोर कमी और काला बाज़ारी का फलता फूलता व्यापार तथा विषम परिस्थितियों में एक दूसरे के काम आते लोग– उस समय की न जाने कितनी घटना, परिघटना, दुर्घटना ,हादसा, सान्हा, वाक़या की चित्रकारी, उनके चलचित्र इस संग्रह की लघुकथाएं बड़ी ही तटस्थता और मार्मिकता के साथ पेश करती हैं। ये कहानियां मानव मन के जज़्बात और अहसासात की कहानियां हैं और अपने विषय एवं कथानक के एतबार से वैविध्य और परतदार।
अफ़सांचा (मोख़्तसर अफ़साना, मिनी अफ़साना या लघुकथा) हर भाषा के साहित्य की एक विशेष विधा है जो औद्योगिक क्रांति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास और उसकी तेज़ रफ़्तार के साथ तालमेल बैठाने के दबाव में भागती-दौड़ती-हांफती ज़िन्दगी, वक्त़ की तंगी और ज़रूरतें पूरी करने की हड़बड़ी में कहानी कहने और सुनने की आदिम जिज्ञासा और जिजीविषा के कारण हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बनी है और लगातार विकसित हो रही है। आज के समय में यह एक लोकप्रिय विधा का दर्जा हासिल कर चुकी है। संक्षिप्त विवरण, सुक्ष्म अवलोकन, विषय का महत्व, किसी एक क्षण, वाक़या, घटना या हादसा का सम्पूर्ण एवं समावेशी विवरण एवं अभिव्यक्ति, व्यंग्य की तीखी धार तथा पंचलाइन का हमारे मन व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव इस विधा की कुछ विशिष्टता हैं। गति और संक्षिप्त विवरण इसके गुण हैं और इसके गठन एवं गढ़न में हमारी गहरी अनुभूति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
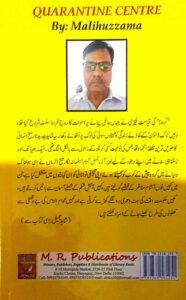
संग्रह की अधिकांश लघुकथाएं इन कसौटियों पर खरी उतरती हैं। कहानी के कथन में छोटे-छोटे वाक्य इसे गहने का काम करते हैं और इसके प्रभाव को कई गुणा बढ़ा देते हैं। भाषा को हम हिन्दुस्तानी कहने में सच के साथ होंगे। इसलिए ये लघुकथाएं हिन्दी भाषी और उर्दू भाषी दोनों के लिए सुगम, सरल और सहज हैं। कहानी की पंचलाइन स्पेशल इफेक्ट पैदा करने में सफल है। विषय का चुनाव जनपक्षधरता और सामाजिक प्रतिबद्धता की मिसाल है और वैविध्य के रंग में रंगा हुआ है। ये लघुकथाएं एक संक्षिप्त काल की हैं, फिर भी लेखक ने परिस्थितियों, विचारों और बयान करने की कला को दोहराने से बचने की सावधानी बरती है। इस वजह से कहानी का प्रवाह और उसकी रोचकता अंत तक बनी रहती है। इन्हें पढ़ते हुए पाठक महामारी की विभिषिका, मानव त्रासदी और विपदा, बाज़ार की मुनाफे की भूख तथा पूंजी के खेल के, ऐसे बवंडर में फंस जाता है कि समय का तूफ़ान उसे दर्द और पीड़ा के उस सैलाब में धकेल देता है जहां वह बेबस एवं लाचार जीने की लड़ाई लड़ता हुआ अंजान मंजिलों की ओर बहा चला जाता है।
यहां संग्रह की सभी लघु कथाओं की अलग-अलग समीक्षा एवं मूल्यांकन संभव नहीं है, फिर भी कुछ लघु कथाओं की संक्षिप्त चर्चा संपूर्णता में इनके प्रभाव के मूल्यांकन में मददगार हो सकती है। इस लिहाज़ से संग्रह की चंद कथाओं का विश्लेषण प्रस्तुत है।
“दायमी सफ़र” अर्थात “अनवरत यात्रा” अपने घरों को बे-सरो-समानी की हालत में छोड़ अपने घरों के लिए विपरीत पलायन करते मज़दूरों-कारीगरों की कहानी है जो रेल की पटरी पर सोते हुए स्पेशल ट्रेन की चपेट में आकर घर पहुंचने के बजाय न ख़त्म होने वाले सफ़र पर चले जाते हैं। कहानी की पंचलाइन बहुत कुछ बयां कर जाती है।
“पटरियों पर बड़ी तादाद में सूखी रोटियां भी बिखरी पड़ी हैं। इन्हीं रोटियों की खातिर उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो गईं।”
बिखरी सूखी रोटियों की इमेजरी बहुत गहरे हमें बेधती है और पूछती है, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार?
लघुकथा “फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग” समाज के ऐसे तब्क़े की कहानी है जो जीवनयापन के लिए अपना शरीर बेचने को अभिशप्त है। यह समाज का सबसे उपेक्षित तब्क़ा है। कोविड महामारी की मार इस पर कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। काम-धंधा बंद है, भूखों मरने की हालत है। ऐसे में सीढ़ियों पर क़दमों की चाप सुनाई पड़ती है। एक उम्मीद जगती है, आंखों में और चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उस व्यक्ति और मालकिन के बीच का संवाद हमें प्रश्नों के घेरे में डाल देता है।
“रत्ना बाई अजनबी से हम कलाम है। नाम क्या है? यहां किस लिए आये हैं? यह शरीफों की जगह तो नहीं? उसके चेहरे पर एक रंग आता है।वह मतानत से जवाब देता है।
“बाई जी नाम में क्या रखा है? रह गया दूसरे सवाल का जवाब तो मैं सुकून की तलाश में आया हूं। मुझे निर्वाण की तलब नहीं है।”
आगे उसने बड़े फ़लसिफ़याना अंदाज़ में कहा – आदमी की सोच गंदी होती है, जगह नहीं।
महामारी से उत्पन्न विपदा की घड़ी में यह कहानी नैतिकता के नये मानदंड की मांग करती है।
एक और लघुकथा “लिन्चिंग” में कोविड काल में क़ानून और प्रशासन के द्वारा चुनिंदा व्यवहार की सच्चाई को उजागर किया गया है।
“कोई एफ़.आई.आर.नहीं, कोई केस नहीं, मामला रफा-दफा कर दिया। भीड़ ने नौजवान का लिंच करते हुए विडियो भी वायरल कर दिया। नौजवान मरते -मरते बचा।”
कहानी स्पष्ट कहती है कि माहौल ऐसा बनाया गया है कि जो पीड़ित है,वहीं दोषी भी है।
एक और लघुकथा “बवंडर” में कोरोना महामारी के दौरान बिल्कुल नई स्थिति और समस्या को संबोधित किया गया है और वह है महामारी में मरने वाले/वाली को दफ़न करने या उसके अंतिम संस्कार करने संबंधी समस्या की।
“आख़िर में आठ- दस घंटों की मेहनत और कोशिशों के बाद बच्चा क़ब्रिस्तान में रात को ढाई- तीन बजे तदफ़ीन अम्ल में आई।”
सिर्फ ज़िन्दगी ही नहीं, मौत भी परेशानियों में घिरी हुई है।
संग्रह की लघुकथा “दहशत” में एक अलग ही दृश्य है। यह दो कबीलों के सरदार के बीच की लड़ाई को दोनों कबीले की लड़ाई में बदलने की कहानी है। वैसे तो यह काल्पनिक कहानी लगती है, पर यह अपने कथन में प्रतीकात्मक है। इसलिए संकेतों में बात करती है। जब सीधे-सीधे बयान करने का जोखिम हद से बढ़ जाए तो प्रतीक का प्रयोग ज़रूरी हो जाता है। इस कहानी में एक कबीले का सरदार दूसरे कबीले के प्रति अपने पूर्वाग्रह और द्वेष के कारण यह प्रचारित करवा देता है कि दूसरे कबीले के लोग एक ऐसी महामारी फैला रहे हैं जिससे हमारा अपना अस्तित्व ख़त्म हो जायेगा। इसलिए उन्हें सबक़ सिखाना ज़रूरी है। हर तरफ महामारी की दहशत फ़ैल जाती है और फिर वही होता है जो सरदार चाहता है।
“ख़तरनाक बीमारी जिसका डर दिखाया गया था, उसका कहीं वजूद नहीं था। यह तो सरदार की एक लाइन थी।”
यह कहानी हम और वे की बायनरी और उत्तर सत्य की मारक शक्ति को भली-भांति रेखांकित करती है तथा यह भी बताती है कि अफ़वाह ध्रुवीकरण की राजनीति को किस तरह आभासी दुश्मन के विरुद्ध इस्तेमाल करने में सफल है।
संग्रह की लघुकथा “फ़ासले” की चर्चा करना कोरोना काल के एक और आख्यान को परत दर परत खोलने के लिए ज़रूरी जान पड़ता है। यह कोरोना काल का वह पड़ाव है जहां यह प्रचारित किया जाता है कि एक खास समुदाय के लोग इसे जानबूझकर फैला रहे हैं और लोगों की ज़िन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुरक्षित दूरी की जगह फ़िज़िकल दूरी गाइडलाइंस का हिस्सा है। ऐसे में शमीम को ऑफिस आने से मना कर दिया जाता है जबकि वह कोरोना निगेटिव है। ऐसे में शमीम का मानसिक द्वंद, उसकी बेचैनी और परेशानी कहानी को आगे बढ़ाती है।
“असिस्टेंट डायरेक्टर ने इस मामले में अपनी लाइलमी ज़ाहिर करते हुए कहा – शमीम बाबू आराम से घर पर रहिए न। कौन आपका पे काट रहा है। मैं हूं न आपके साथ। सिलसिला मुन्क़ता हो गया।”
सामाजिक पूर्वाग्रह और अंधविश्वास किस हद तक घिर गया है, यह साफ़-साफ़ झलकता है।
यहां एक और लघुकथा की चर्चा ज़रूरी है। एक तरफ़ महामारी का डर, दूसरी तरफ़ भूख प्यास का डर, हर तरफ़ जान का डर। ऐसे में जीने के लिए भूख मिटाने का संघर्ष।
“बाहर जमेग़फ़ीर है। किसी फ़लाही तंज़ीम ने खाने का इंतजाम किया है। वह गिरते पड़ते वहां पहुंच जाता है और क़तार में लग जाता है। जब घंटों बाद उसका नंबर आता है तो ग़श खाकर गिर जाता है।”
एक ऐसे माहौल का चित्रण जहां ज़िन्दा रहने का संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है।
“हनीमून” विषेयक लघुकथा वैसे तो पारिवारिक कलह की कविता लगती है, पर महामारी और लाॅकडाउन ने इसे विस्तार दिया है और संवेदनात्मक धरातल पर इसकी जटिलता को उजागर किया है।
“रात के आठ बजे वज़ीर आज़म ने लाॅकडाउन का एलान कर दिया और हनीमून अल्तवा में चला गया। आमना बीबी के चेहरे पर मायनीख़ेज़ मुस्कुराहट रक़्स कर रही थी।”
यह कहानी सास-बहू के झगड़े के मनोवैज्ञानिक पहलू को खोलती है जहां सास आपदा को अवसर में बदलते देख ख़ुश होती है। यह भी एक प्रतीक है।
“साज़िशी” महामारी के एक अलग पहलू की कहानी है जो एक डाक्टर के सामाजिक पूर्वाग्रह का शिकार होने और सामुदायिक क्लेश को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को दर्शाता है।
“वह मुझ पर भड़क गई और ग़ुस्सा से तमतमाते हुए कहने लगी। क्या आप लेफ़्टिस्ट हैं या अर्बन नक्सल जो इस क़िस्म की देशद्रोही बातें पूछ रहे हैं। उठिए, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगी।”
किस तरह विभेद, विभाजन और नफ़रत की सियासत अपना दुश्मन गढ़ती है और समाज के लिए ख़तरनाक हो जाती है, इस कहानी का स्पष्ट संदेश है।
कहानी “खुशबूओं की बारात” एक और अलग तरह की समस्या हमारे सामने लाती है। शादी के दिन ही लाॅकडाउन की घोषणा हो जाती है। दुल्हा, दुल्हन और बाराती सब फंस जाते हैं। दुल्हन के घर वालों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। किसी तरह समुदाय और प्रशासन की मदद से समस्या हल होती है।
“इकहत्तर दिनों के बाद दुल्हन ने हिन्दू रीति रिवाज के मुताबिक गृह प्रवेश किया।”
यह कहानी आपसी समझदारी, परस्पर सहयोग और सद्भाव की कहानी है।
कहानी “ड्रामे बाजियां” समाज की एक और कड़वी सच्चाई को उजागर करती है।
“थाली नहीं पीटी तो पड़ोसियों ने वायकाट कर दिया। घर को आठ मिनट तक अंधेरा कर बालकोनी में चिराग़ां नहीं किया तो मेरी वतन परस्ती मशकूक कर दी गई और मेरी पहचान को एक्सपोज़ कर दिया गया। मेरे ग़ैर मुस्लिम साथी मुझसे किनारा करने लगे। पर्ब त्योहार में नेक ख़वाहिशात के जो मेसेज आते थे,वह बंद हो गये। मुझसे एक ख़ास क़िस्म की दूरी बना ली गई। यों जैसे कि मैं कोई अछूत हूं।”
एक और कहानी “कठिन डगर” की चर्चा के बिना बात पूरी नहीं होगी। यह कहानी कोरोना काल में चलाई गई ‘श्रमिक स्पेशल’ की बदहाली और बदइंतज़ामी की गाथा है।
“तीसरे दिन लंच मिला। कुछ राहत का एहसास हुआ। ट्रेन कब पहुंचेगी, किसी को कोई अंदाजा नहीं। पांचवें दिन ट्रेन पटना पहुंचती है। तीन दिन की ताख़ीर से। और बच्चा मां की गोद में दम तोड़ चुका था।”
बाक़ी कहानियों का भी बयानीया अलग-अलग हालात की अक्कासी है। इस तरह संग्रह की लघुकथाएं हमारे अपने आस-पास की हमारी अपनी कहानियां हैं। हम इन कहानियों से बार-बार गुज़रे हैं। हम ने इन्हें झेला है। कोरोना काल की हर ख़बर, अख़बार की हर सुर्ख़ी लघुकथा का विषय भी है और उसके लिए कच्चा माल भी। फिर लेखक का अपना नज़रिया, उसकी विश्वदृष्टि , उसकी कल्पना शक्ति और उसका संवेदनात्मक आवेग– यह सब मिलकर कहानी को अच्छी कहानी बनाने में सफल हैं। यह संग्रह पठनीय संग्रह बन पाया है और गंभीर चर्चा की दावत देता है।
(समीक्षित पुस्तक : क्वारंटाइन सेन्टर (कोविड-19 के संबंध में लिखी गई लघुकथाएं); पुस्तक की भाषा : उर्दू , कथाकार : मलीहुज़्ज़मां, प्रथम संस्करण : 2024, एम. आर. पब्लिकेशन, दरिया गंज, नई दिल्ली)
9431151332
drkhan.principal@gmail.com







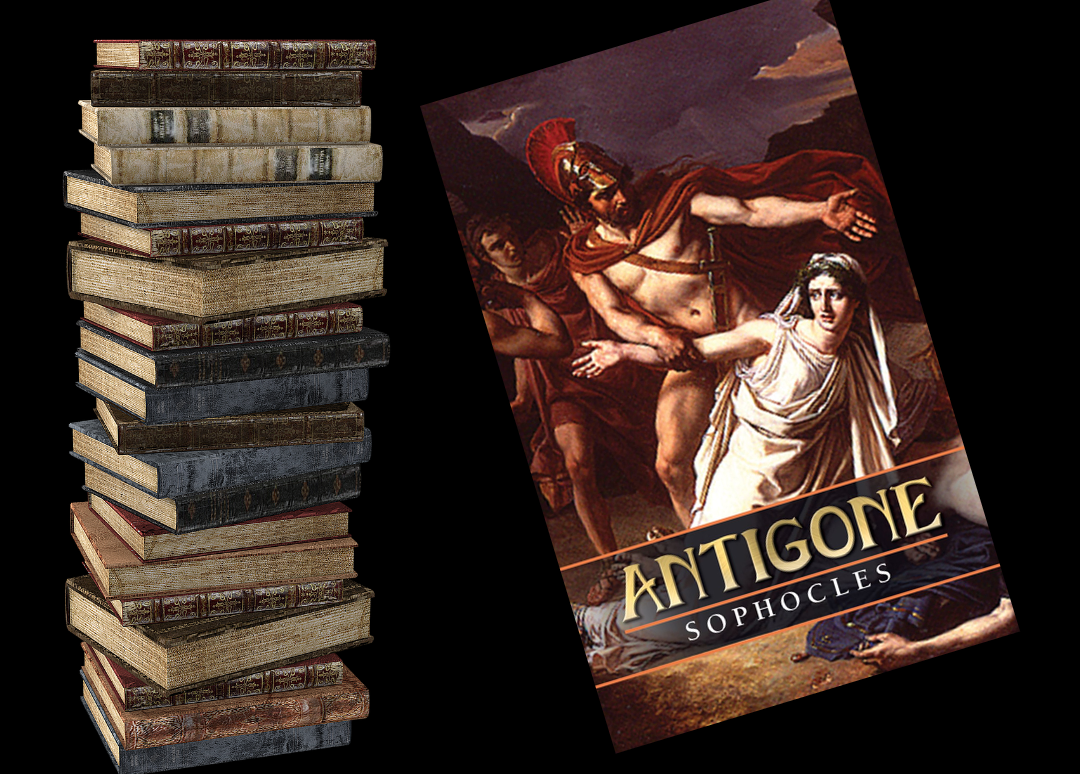

अच्छी समीक्षा है
जरूरी किताब और सार्थक समीक्षा ।