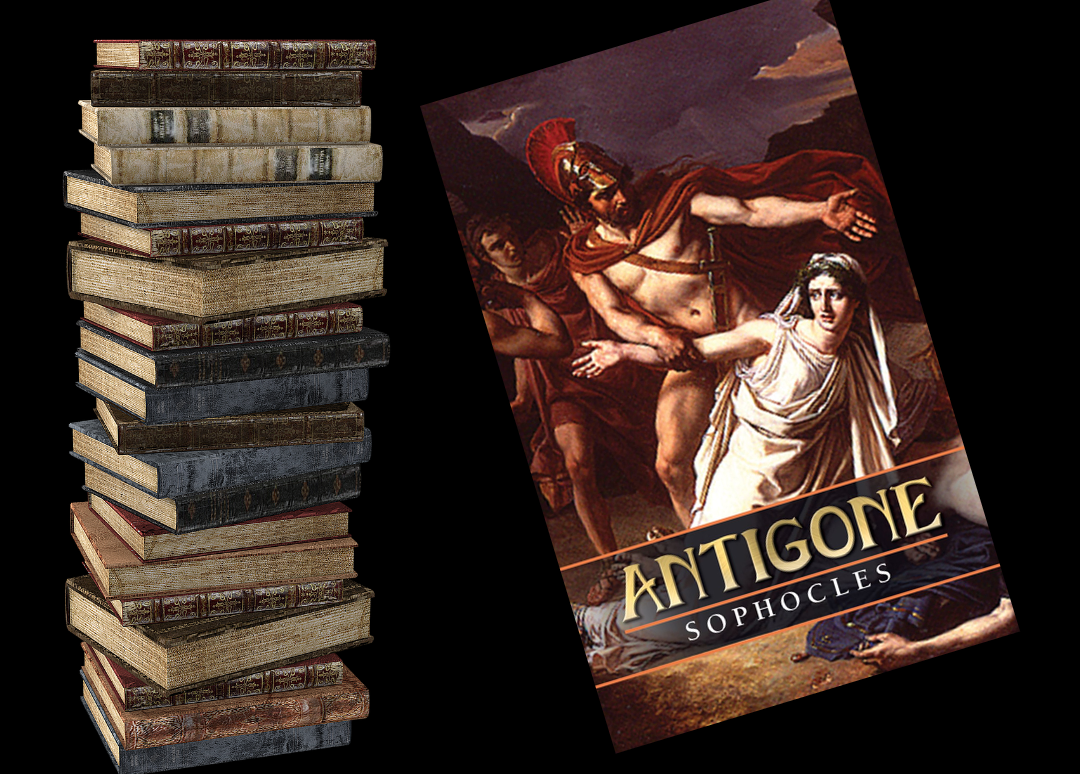शंकर दयाल सिंह (1937–1995) एक प्रखर कांग्रेस नेता, विद्वान स्तंभकार और हिंदी के सजग प्रहरी थे। 33 वर्ष की आयु में वे लोकसभा सांसद बने और बाद में राज्यसभा में भी उल्लेखनीय भूमिका निभायी। उन्होंने 30 से अधिक किताबें लिखीं जिनमें यात्रा-वृत्तांत, संस्मरण और राजनीतिक लेख प्रमुख हैं। ‘धर्मयुग’, ‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ जैसी पत्रिकाओं में उनके स्तंभ अत्यंत लोकप्रिय रहे। पटना में पारिजात प्रकाशन की स्थापना कर उन्होंने ग्रामीण भारत में साहित्यिक चेतना का प्रसार किया। ‘इमर्जेंसी: क्या सच, क्या झूठ’ उनकी चर्चित कृति रही। उन्हें ‘बिहार रत्न’ और ‘अनंत गोपाल शेवड़े हिन्दी सम्मान’ जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। 1995 में उनका निधन हुआ। उनकी स्मृति में आज भी व्याख्यानमालाएँ और पुरस्कार जारी हैं, जो उनकी बहुआयामी विरासत को जीवित रखते हैं।–मोहम्मद नौशाद, पीएचडी-राजनीति विज्ञान
——————————————–
दिल्ली पिछले दिनों कुल मिलाकर छह साल रहा और वह भी एक संसद सदस्य के रूप में। और संसद सदस्य का रौब-दाब क्या होता है, कौन-कौन सी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती हैं, आसमान-ज़मीन पर चलने-उड़ने का उन्हें कौन-कौन सा अधिकार प्राप्त रहता है, वे वही जानते है जो एक बार संसद सदस्य रह चुके होते हैं। और एक बार जब कोई संसद सदस्य हो जाये तो उसके बाद और कुछ वह न तो होना चाहता है और न उस पद प्रतिष्ठा से हटना चाहता है। इसलिये स्व० राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अक्सर मुझसे कहा करते थे कि एम० पी० गिरी छोड़कर मैंने वाइस-चांसलरी स्वीकार की थी, दुनिया में इससे बड़ी बेवक़ूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती है!
श्री अजीत प्रसाद जैन ने तो केरल का राज्यपाल पद छोड़ दिया था, केवल ए० पी० रहने के लिए और इसी प्रकार न जाने कितने उदाहरण हमारे सामने और हैं। वही एम० पी० पद मुझे भी मिला—मात्र छह वर्षों के लिये और इन छह वर्षों की ओर देखकर अब सोचता हूँ तो लगता है मानो या तो वे मिले ही न होते और यदि मिल गये तो फिर छूटे न होते। कहाँ सारे देश में वायुयान और रेलगाड़ी की पूरी सुविधा, कहीं भी जाओ तो सर्किट हाऊस में मात्र एक-दो रुपये बिजली चार्ज देकर रिजर्वेशन, फिर स्टेट गैस्ट, जिस कमेटी की मीटिंग मे जाओ, उस विभाग के अफ़सरों का एक पाँव पर खड़े रहना, संसदीय मीटिंगों में भाग लेने अथवा संसद-सत्र में भाग लेने के लिये 51.00 रुपये रोज़ का भत्ता, बैठकों और सत्रों में भाग के लिये आने-जाने में रेल पास के अतिरिक्त भी एक प्रथम श्रेणी और एक द्वितीय श्रेणी का अतिरिक्त किराया, संसद सत्र के समय पत्नी के साथ आने-जाने का रेल ‘पास’ के अतिरिक्त रेल में एक द्वितीय श्रेणी का साथ के सज्जन के लिये भी पास! दिल्ली में रहने के लिये बंगला, सेंट्रल हॉल की मंद मंद हवा; वहीं चाय-कॉफी-नाश्ता, खाना सबों की किफ़ायती दामों में व्यवस्था। रेल का आरक्षण हो या हवाई जहाज का, संसद भवन से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बैंक और पोस्ट ऑफ़िस भी संसद भवन के अन्दर ही, बंगले या फ्लैट का किराया किफ़ायती से भी किफ़ायती, बिजली-पानी-फर्नीचर-सफ़ाई किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो फोन करते ही आदमी हाज़िर; दिल्ली और अपने निवास पर भी फोन की सुविधा, अनेकानेक कमेटियों में रहने पर रौब-दाब और दबदबा, किसी भी अधिकारी को फोन उठाकर कह देना ही उसकी कुर्सी हिला देने के लिये काफ़ी, साल दो साल में विदेश जाने की भी सुविधा। भला इन बातों की याद किसी भी भूतपूर्व संसद सदस्य को आती होगी, तो रात की नींद तो जरूर हराम हो जाती होगी!
मैं तो मात्र छः साल एम० पी० रहा, इसलिये कुछ हद तक सम्भल भी गया, लेकिन उनका हाल क्या होता होगा, जो 20 साल, 25 साल 27 साल से लगातार एम० पी० थे। मेरी समझ में उनका दुःख और उनकी पीड़ा मेरे जैसे लोगों से पाँच-छह गुनी अधिक होगी। और उन बेचारे मन्त्रियों का हाल क्या होता होगा जो बिना पी० ए० न तो चल पाते थे, न फोन कर पाते थे, न गाड़ी का दरवाज़ा खोल पाते थे, और न एक फाइल स्वयं अपने हाथों उठा पाते थे। उनमें भी जो लगातार दस बीस, पच्चीस साल मंत्री रह गये, उनका हाल तो ओर बेहाल होगा।
मुझे जब कभी कोई भूतपूर्व मंत्री या भूतपूर्व ससंद सदस्य मिल जाते है, तो बड़े करीने से यह सवाल उनसे पूछता हूँ कि वे दिन जब याद आते हैं, तो आपको कैसा लगता है ? बहुत सारे तो अपनी झेंप मिटाने के लिये हैं हैं…..हां… हां… करते हुये कह देते हैं- मुझे तो कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा है। ज्यों का त्यों हूँ। कुछ लोग इस प्रकार हैं भी, लेकिन कई लोगों के पिचके गाल, उदास चेहरे, परेशानी से भरा जिस्म देखकर उनके संकट का अन्दाज हो जाता है और दया उमड़ पड़ती है।
बहुत से ऐसे भी होते हैं, जो बेचारे ईमानदारी से अपनी बातें कह देते हैं, ‘भाई, परेशानी-ही-परेशानी है। कहाँ दिल्ली की मौजभरी ज़िंदगी और कहाँ अपने क़स्बे का भिनभिनाता जीवन। पर करें क्या? जनतंत्र में जो भी फ़ैसला हो, मानना चाहिए, आख़िर गये भी तो थे हम उन्हीं की बदौलत । अब फिर पाँच साल बाद पहुँचेंगे। ये बातें आत्मविश्वास की भी है और सही भी !
+ + + + + + + + +
एक भूतपूर्व मंत्री मिले तो, घुमा फिरा कर मैंने उनसे यही सवाल किया, बेचारे बड़ी इमानदारी में बोले- भाई साहब, आप से क्या छुपाऊँ! घर से बाहर निकलने में भी लाज आती है, पिछले दस साल तक मंत्री रहा, जाना ही नहीं कैसे कौन काम होता है। जो जानता भी था, वह भी पी० ए० और पी० एस० के फेर में भूल गया! यहाँ तो नौबत यह है कि लोग आजकल मिलने जुलने में भी कतराते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि चुनाव वाली जीप से जा रहा था। ठीक बाज़ार में वह बंद हो गई। ड्राइवर ने कहा कि बिना ठेले स्टार्ट नहीं होगी। मैं नीचे उतर कर सिर नीचा कर ठेलने लगा कि शायद दो चार लोग आकर लग जायेंगे, लेकिन जिस शहर में कभी मेरे स्वागत में बदनवार सजाये गये थे, हर आदमी माला लेकर गले में डालने को आतुर था, जय-जयकारों से आसमान गूँज उठा, उसी में यह हालत थी कि एक आदमी मेरी गाड़ी में हाथ लगाने को भी तैयार नहीं था। उन्होंने एक लम्बी साँस ली, मैंने अपने मन में कहा, यही तो जनतन्त्र है!
एक मंत्री महोदय मिले। जो तीन-चार साल ही मंत्री रह पाये थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की आँख बचाकर भाग जायें, लेकिन मैं कहाँ छोड़ने वाला था, लपक कर मैंने उन्हें पकड़ा, “भाई साहब, क्या हाल-चाल है, कहाँ हैं आजकल, क्या कर रहे हैं?”
खादी ग्रामोद्योग के पास रीगल की बगल में वे मिल गये थे, बोले- “बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का सबसे मुश्किल सवाल है, मैं तो रात-दिन कोई किराये के मकान खोजने में ही लगा हूँ, अब तक कोई मकान नहीं मिल पाया है।”
मैंने पूछा- “तो आख़िर हैं कहाँ, यहाँ?”
उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बात टल जाये, लेकिन मैं छोड़ने वाला कहाँ था। अन्त में उनके मुँह से बात निकलवा ही ली। मायूसी के साथ बोले- “क्या करता, वो जो भूतपूर्व एम० पी० है न, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपना बंगला अभी नहीं छोड़ा है, उन्हीं के आउट हाउस में तत्काल मैं हूँ। लेकिन बड़ी तकलीफ़ है।”
+ + + + + +
लेकिन अपनी ही बात अब अधिक कहूँ । रह-रह कर दिल्ली और एम० पी० गिरी याद आती है। सुख के सुविधाओं में रह कर आदमी भूला रहता है, खोया रहता है, बराबर दिमाग़ आसमान पर रहता है। कुछ वैसा ही हाल रहा, लेकिन ख़ुशी की बात यही रही कि ज़मीन से संबंध नहीं छूटा था, इसलिए तकलीफ़ की मात्रा कुछ कम रही। वैसे दिल्ली इसलिए और भी याद आती है कि वहाँ मित्रों-हितैषियों-शुभेच्छुकों का बहुत बड़ा क़ाफ़िला तैयार हो गया था। साहित्यिक-सांस्कृतिक वातावरण बन गया था, सारे भारत के लोगों से सम्पर्क हो गया था। राजधानी की अपनी रंगीनी ही और होती है; उस चकाचौंध से भला कौन ऐसा होगा, जो न रंग जाये !
दिल्ली से हटने के बाद इन दिनों पटना में हूँ। यह भी एक बड़ा शहर है, बिहार प्रांत की राजधानी- कभी यह नगर मौर्यों का केन्द्र बिंदु था। चन्द्रगुप्त और अशोक सब हुए यहीं। यहाँ और इसके आसपास भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के चरणों की थाप भी है- लेकिन इन सबके बाबजूद उस समय भी हस्तिनापुर या दिल्ली का रौबदाब कुछ अपना ही था; और आज भी कुछ अपना ही है। कहाँ वे कचकचाती हुई सड़कें, कहाँ वे आसमान को छूने वाले भवन, कहाँ कनाट प्लेस और जनपथ की रौनक, कहाँ बुद्ध पार्क और नेहरू पार्क की हवा, कहाँ राजघाट की दूव और शान्तिवन के गुलाब, कहाँ राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट की मीनार, कहाँ जगह-जगह झरनों और फूलों और पार्कों की भरमार, कहाँ विभिन्न दूतावासों की दावतें, कहाँ एक से अनेक राजनीतिक सरगर्मियाँ और कहाँ मानचित्र के किसी कोने में दुबका हुआ-सा बेचारा यह शहर पटना । दोनों में ज़मीन और आसमान का अन्तर है। इसलिये तो रह-रहकर दिल्ली याद आती है।
वहाँ आँखें खुली नहीं कि अख़बार हाज़िर और यहाँ इंतज़ार करते-करते आँखें पथरा जाती हैं और समाचार जब पुराने होने लगते हैं, तब अख़बार वाले की साइकिल पहुँचती हैं। वहाँ बच्चों की पढ़ाई का एक स्वस्थ सिलसिला, बसें और पढ़ाई का स्तर हर जगह से सन्तोषप्रद, और यहाँ हफ़्ते में तीन दिन स्कूल-कॉलेजों में हड़ताल और सम्पूर्ण-क्रान्ति की गूँज ।
भला ऐसी स्थिति में दिल्ली क्यों न याद आये। अब तो भूलने लगा हूँ कि अशोक, अकबर और ओवेरॉय नाम का कोई होटल भी है इस देश में। कभी-कभी मोतीमहल का ज़ाइक़ा याद आता है तो लार टपकती है। और सब तो सब कहीं मिल भी जाये, लेकिन इंडिया गेट की शाम और मदमाती हवा शायद ही कहीं मिले, वे खोमचे वाले, आइसक्रीम वाले, घासों पर पड़े-पड़े रोमांस करने वाले और बिना किसी काम यों ही चहलक़दमी करने वाले जोड़े न भूलते हैं, न भुलाये जा सकते हैं।
इसलिए तो रह-रहकर वे दिन याद आते हैं- सपनों में भी और सिहरनों में भी। अनुभूतियों में भी और जिज्ञासाओं में भी। पता नहीं अब कभी दिल्ली पहुँचना होता है या नहीं- उस रूप में जिस रूप में दिल्ली में विगतः छह वर्षों तक रहा। अभी भी दिल्ली प्रायः आता-जाता रहता हूँ , लेकिन स्टेशन से जब कोई टैक्सी या स्कूटर लेकर आगे बढ़ता हूँ और उसका ड्राइवर यह पूछता है कि साहब कहाँ चलना है, तो मुँह से बरबस वे ही पुराने खेमे याद हो आते हैं-मीनाबाग और फ़िरोज़शाह रोड और आवाज़ एक कसक बनकर रह जाती है।
संदर्भ- कुछ बातें: कुछ लोग
पृष्ठ संख्या: 34-37